दर्शन क्या है?
मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सोचने की क्षमता मनुष्य का ऐसा गुण है जो उसे अन्य जीवों से अलग करता है। Aristotle ने मनुष्य को “विवेकशील प्राणी” कहकर उसकी बुद्धिमत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया है। विवेक यानी बुद्धि की प्रधानता, जिसके बल पर मनुष्य विश्व की विभिन्न वस्तुओं को समझने और उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करता है।
मनुष्य की बौद्धिकता उसे जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रेरित करती है, जैसे:
- विश्व का स्वरूप क्या है?
- विश्व की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई?
- ईश्वर है या नहीं?
- आत्मा और जीव का स्वरूप क्या है?
- जीवन का चरम लक्ष्य क्या है?
- ज्ञान और नैतिकता का आधार क्या है?
इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की इस प्रक्रिया को ही दर्शन कहते हैं। दर्शन के माध्यम से व्यक्ति तर्क और बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन गूढ़ प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसी कारण दर्शन को ‘फिलॉसफी’ भी कहा जाता है, जो ग्रीक शब्दों “फिलोस” (प्रेम) और “सोफिया” (ज्ञान) से मिलकर बना है।
भारतीय दर्शन: अनुभव और साक्षात्कार का अद्भुत संगम
भारत में दर्शन का अर्थ “जिसके द्वारा देखा जाए” से है। भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि तत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसका प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय विचारधारा के अनुसार, तत्व का साक्षात्कार दो प्रकार की अनुभूतियों से संभव है:
- ऐंद्रिय अनुभूति (Sensuous Experience): जिसे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
- अनैंद्रिय अनुभूति (Non-sensuous Experience): जिसे आध्यात्मिक अनुभूति कहा जाता है।
भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक अनुभूति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है क्योंकि यह बुद्धि के स्तर से परे होती है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का द्वैत समाप्त हो जाता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, यह अनुभूति ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है, और इसी कारण इसे “तत्व दर्शन” कहा जाता है।
भारतीय दर्शन की विशेषताएं
-
व्यावहारिकता:
भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल जिज्ञासा शांत करना नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। जब मनुष्य ने अपने को दुःख और क्लेश से घिरा पाया, तब उसने उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए दर्शन का सहारा लिया। प्रो. हिरियाना के अनुसार, “पाश्चात्य दर्शन की भाँति भारतीय दर्शन का आरम्भ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर जीवन को नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के शमन के निमित्त हुआ।” -
मोक्ष का लक्ष्य:
भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य “मोक्ष” है, जिसे दुःखों से मुक्ति की अवस्था माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के दुःख समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन को “मोक्ष-दर्शन” भी कहा जाता है। -
आध्यात्मिकता:
भारतीय दर्शन में आत्मा को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आत्मा के स्वरूप का अनुशीलन यह दर्शाता है कि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता की विशेष महत्ता है। इसी कारण इसे कभी-कभी “आत्म विद्या” भी कहा जाता है।
दर्शन का मानव जीवन से संबंध
दर्शन मानवीय स्वभाव का अभिन्न अंग है। यह प्रश्न करना कि “हम दार्शनिक हैं या नहीं,” निरर्थक है, क्योंकि हर मनुष्य किसी न किसी रूप में दार्शनिक होता है। Aldous Huxley का यह कथन महत्वपूर्ण है कि “मनुष्य दार्शनिक और अदार्शनिक में विभाजित नहीं हो सकता; विभाजन केवल कुशल और अकुशल दार्शनिकों का हो सकता है।”
निष्कर्ष
भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता है। यह न केवल जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, बल्कि उन उत्तरों को जीवन में अनुभव करने पर भी बल देता है। ज्ञान की यह यात्रा केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव तक पहुंचने का साधन है।
इसलिए भारतीय दर्शन केवल “ज्ञान का प्रेम” नहीं, बल्कि “जीवन के दुखों से मुक्ति” का मार्ग है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि दुखों से परे एक स्वतंत्र और मोक्षपूर्ण जीवन जीना है।


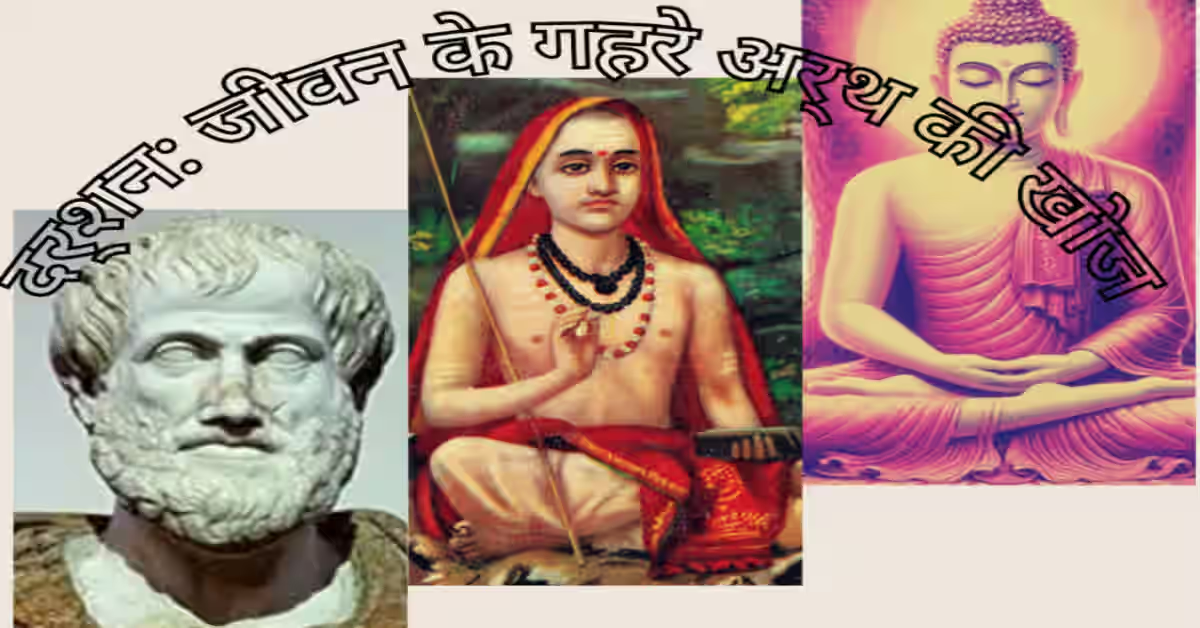
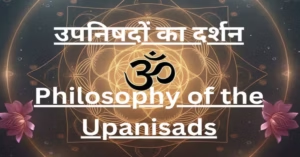
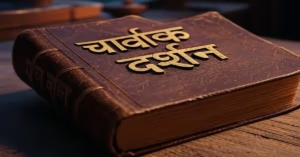
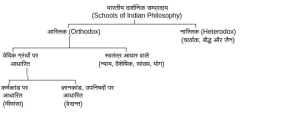
Pingback: चार्वाक दर्शन की समीक्षा: A Critical Review Of Charvaka Philosophy - Shivoham