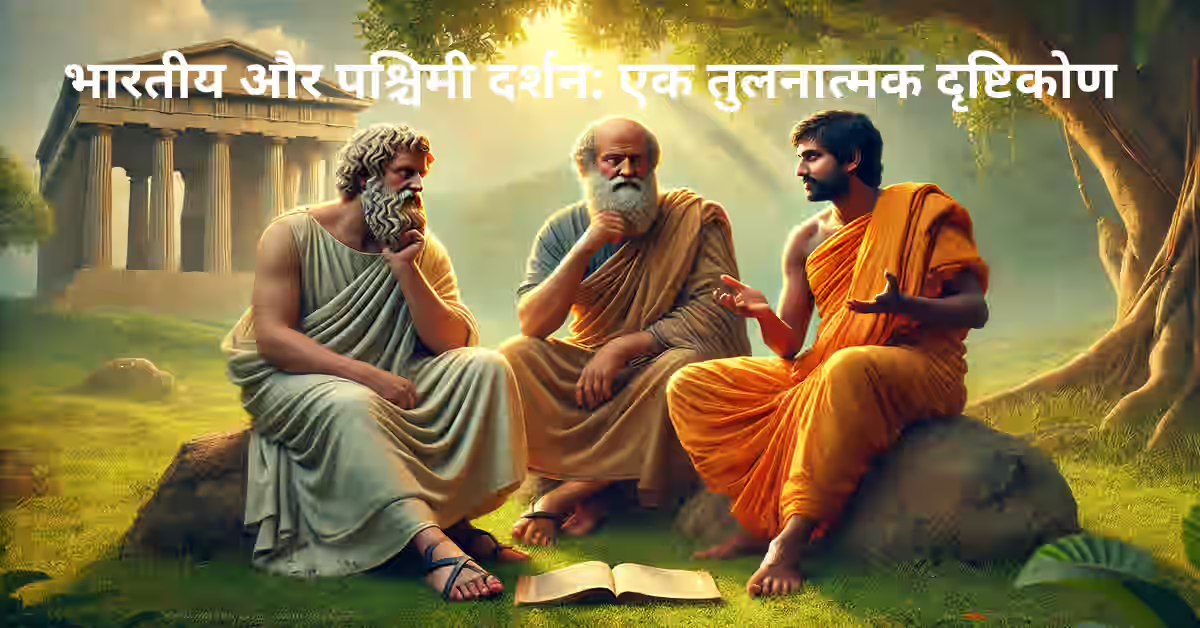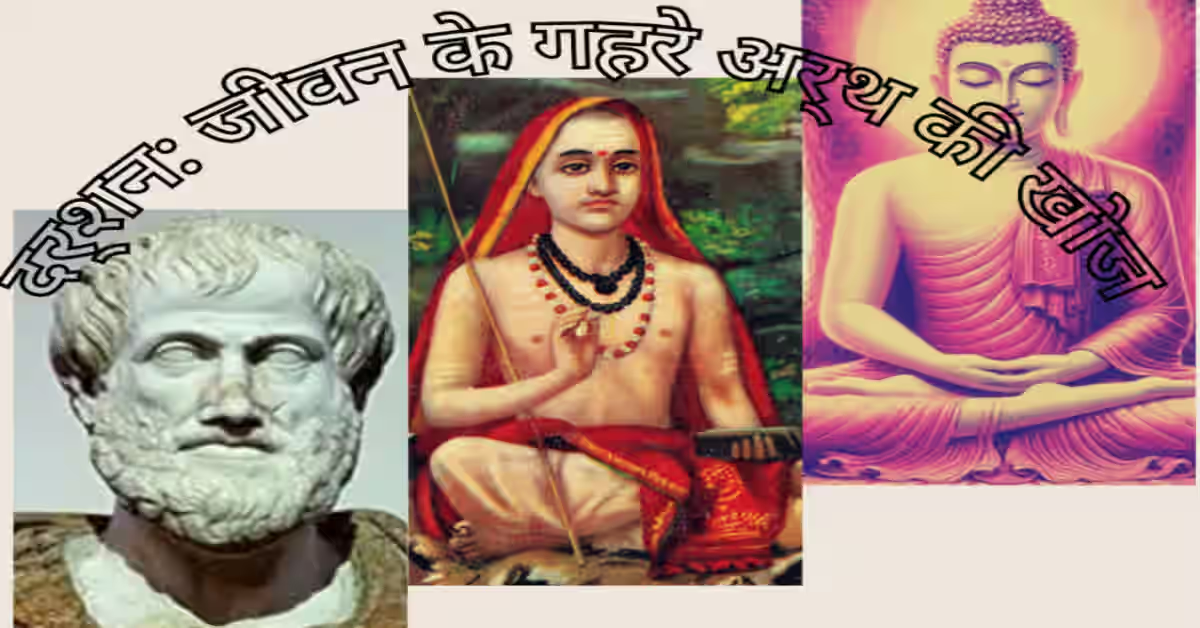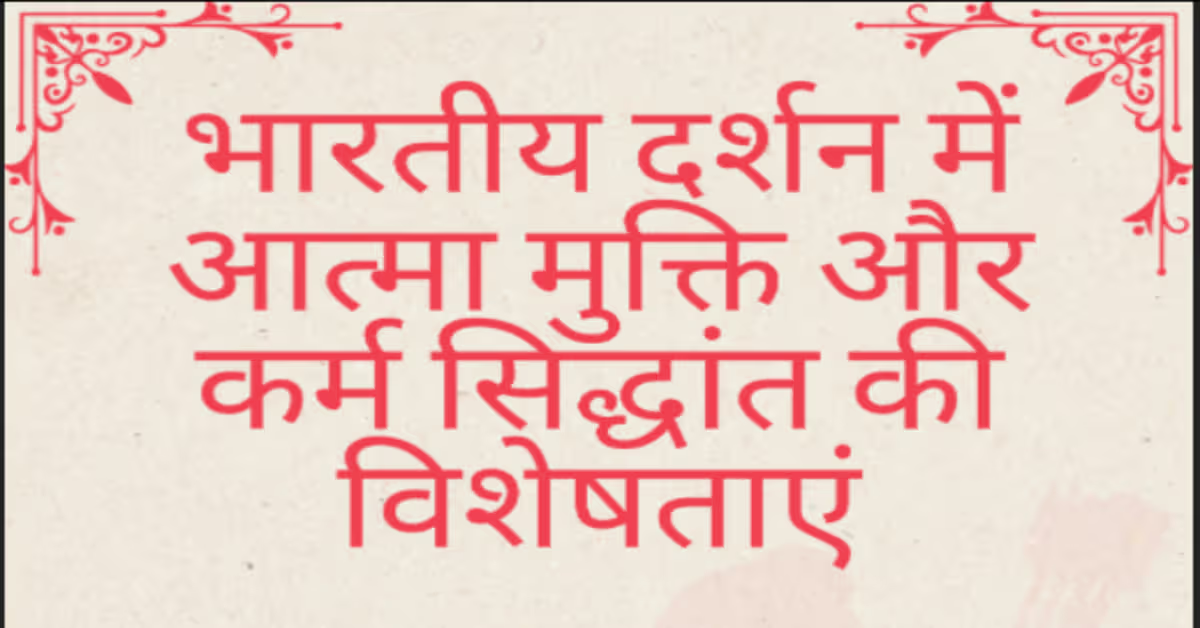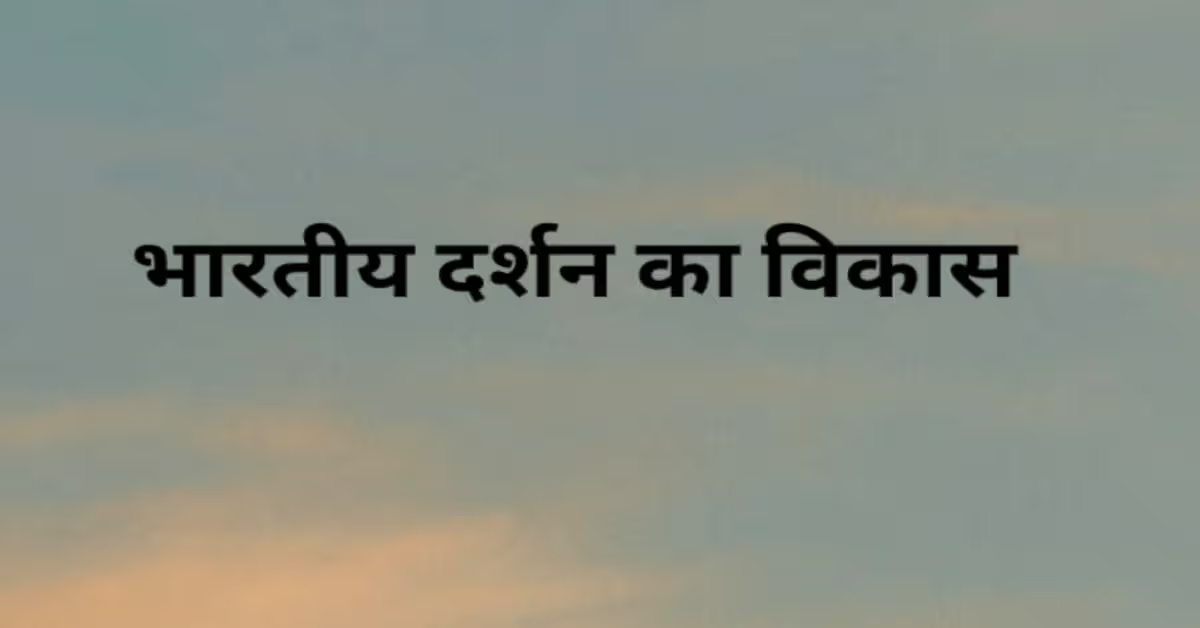हर देश का अपना विशिष्ट दर्शन होता है, जो उस देश की संस्कृति, इतिहास, और जीवन दृष्टि का प्रतिबिंब है। ‘भारतीय दर्शन‘ और ‘पश्चिमी दर्शन‘ का नामकरण ही इस बात का प्रमाण है कि दोनों में मौलिक भिन्नताएं हैं। जबकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है, दर्शन मानवीय दृष्टिकोण और अनुभवों से प्रभावित होकर विषय-निर्भर बनता है। यही कारण है कि भारतीय और पश्चिमी दर्शन अलग दृष्टिकोण और उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं।
भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन: प्रमुख भिन्नताएं
1. दृष्टिकोण: व्यावहारिकता बनाम सैद्धांतिकता
पश्चिमी दर्शन:
- पश्चिमी दर्शन मुख्यतः सैद्धांतिक (theoretical) है।
- इसका आरंभ आश्चर्य और जिज्ञासा से हुआ है।
- पश्चिम में दर्शन को “मानसिक व्यायाम” माना गया है, जिसका उद्देश्य ज्ञान की खोज है।
- यहाँ दर्शन को स्वयं में साध्य (end in itself) माना गया है।
भारतीय दर्शन:
- इसके विपरीत, भारतीय दर्शन व्यावहारिक (practical) है।
- इसका आरंभ आध्यात्मिक असंतोष और दुखों के निवारण की चाह से हुआ।
- भारतीय दर्शन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, जो जीवन के दुखों से मुक्ति की अवस्था है।
- प्रो. मैक्समूलर ने लिखा है, “भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था।
2. ज्ञान की प्रकृति: तार्किक बनाम आध्यात्मिक
पश्चिमी दर्शन:
- पश्चिमी दर्शन बौद्धिक (intellectual) है और इसमें तर्क और विश्लेषण को प्राथमिकता दी गई है।
- डेमोक्राइट्स, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, डेकार्ट आदि दार्शनिकों ने बुद्धि को सत्य ज्ञान का आधार माना।
- बुद्धि के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को परोक्ष (indirect) कहा जाता है।
भारतीय दर्शन:
- भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान (intuitive knowledge) को प्रधानता दी गई है।
- यहाँ सत्य का केवल सैद्धांतिक विवेचन पर्याप्त नहीं माना जाता; सत्य की अनुभूति पर बल दिया गया है।
- आध्यात्मिक ज्ञान को तार्किक ज्ञान से उच्चतर माना गया है क्योंकि इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत समाप्त हो जाता है।
3. धर्म और दर्शन का संबंध
पश्चिमी दर्शन:
- पश्चिमी दर्शन और धर्म का संबंध विरोधात्मक है।
- यहाँ धर्म को व्यावहारिक और दर्शन को सैद्धांतिक माना गया है।
- पश्चिमी दर्शन में धर्म की उपेक्षा की गई है।
भारतीय दर्शन:
- भारतीय दर्शन धर्म से गहराई से प्रभावित है।
- धर्म और दर्शन का सामान्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है।
- धर्म-सम्मत आचरण को सत्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है।
4. संसार के प्रति दृष्टिकोण
पश्चिमी दर्शन:
- पश्चिमी दर्शन इहलोक (this-world) पर केंद्रित है।
- इसके अनुसार, इस संसार के अतिरिक्त कोई अन्य संसार (जैसे स्वर्ग या नरक) नहीं है।
भारतीय दर्शन:
- भारतीय दर्शन परलोक (other-world) में भी विश्वास करता है।
- स्वर्ग और नरक की अवधारणा को यहाँ सभी दर्शनों (चार्वाक को छोड़कर) में स्वीकार किया गया है।
- भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण जीवन और जगत के प्रति दुःखात्मक और अभावात्मक है।
5. विश्लेषणात्मक बनाम संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
पश्चिमी दर्शन:
- इसे विश्लेषणात्मक (analytic) कहा जाता है।
- दर्शन की विभिन्न शाखाओं जैसे तत्व-विज्ञान, नीति-विज्ञान, ईश्वर-विज्ञान आदि की व्याख्या अलग-अलग की गई है।
भारतीय दर्शन:
- भारतीय दृष्टिकोण संश्लेषणात्मक (synthetic) है।
- यहाँ दर्शन की सभी शाखाओं पर एक साथ विचार किया गया है।
- बी.एन. शील ने इसे “संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण” कहा है।
मिलन की संभावना
हालांकि भारतीय और पश्चिमी दर्शन में अनेक भिन्नताएं हैं, लेकिन यह कहना कि इनका मिलन असंभव है, अनुचित होगा।
गत दशकों में भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने “विश्व दर्शन” के निर्माण के प्रयास किए हैं, जो दोनों परंपराओं के सर्वोत्तम पहलुओं का समन्वय करेगा।
विश्व दर्शन के अस्तित्व में आने पर यह भी विज्ञान की तरह सार्वभौम और सर्वमान्य हो सकता है। यह न केवल विभिन्न दृष्टिकोणों को एक मंच पर लाएगा, बल्कि मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य भी करेगा।
निष्कर्ष
भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण अद्वितीय हैं।
- पश्चिमी दर्शन तर्क और बुद्धि पर आधारित है।
- भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता पर केंद्रित है।
दोनों की भिन्नताओं के बावजूद, इनका संगम न केवल संभव है, बल्कि एक नई वैश्विक दार्शनिक दृष्टि की नींव भी रख सकता है। यह समन्वय न केवल दर्शन के क्षेत्र को समृद्ध करेगा, बल्कि मानवता के समग्र विकास में भी योगदान देगा।