भारत के दार्शनिक सम्प्रदायों को आमतौर पर आस्तिक और नास्तिक में विभाजित किया जाता है। आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त शामिल हैं, जबकि नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध और जैन आते हैं। इन दर्शन में भिन्नताएँ तो हैं, लेकिन इनका सामान्य आधार भारतीय संस्कृति और निष्ठा पर आधारित है। सभी में कुछ सामान्य सिद्धांत और प्रामाणिकता पाई जाती है, जिससे भारतीय दर्शन की विशेषताएँ प्रकट होती हैं। इन विशेषताओं का भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है।
मुक्ति (मोक्ष) की अवधारणा (The concept of liberation (moksha))
भारतीय दर्शन का उद्देश्य इस दुःख से मुक्ति है, जिसे ‘मोक्ष’ कहा जाता है। यह मुक्ति विभिन्न मार्गों से प्राप्त की जा सकती है जैसे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, जैन के त्रिमार्ग, या सांख्य और शंकर के ज्ञान के माध्यम से।
हालाँकि भारतीय दर्शन दुःख को स्वीकार करता है, पर यह निराशावादी नहीं है। हर दर्शन दुःख के कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के उपाय प्रस्तुत करता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष, दुःखों से मुक्ति की अवस्था है और इसे जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है।
भारतीय दर्शन में आत्मा (Soul in Indian Philosophy)
यहाँ के अधिकांश दार्शनिक आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं। उपनिषदों और वेदांत में आत्मा की खोज पर जोर दिया गया है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार आत्मा अमर, अविनाशी और निराकार होती है, जबकि शरीर का विनाश होता है।
चार्वाक, जो भौतिकवादी थे, ने आत्मा को शरीर के समान ही माना और उसे नश्वर बताया। वे आत्मा के अमरत्व का नकार करते हैं। बुद्ध ने आत्मा को क्षणिक चेतना का प्रवाह माना और इसे निरंतर बदलता हुआ बताया। उनके विचारों को अनुभववादी (empirical) कहा जाता है।
जैन दर्शन में आत्मा को चैतन्ययुक्त और अनन्त शक्ति से युक्त माना गया है, जिसमें ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद की अनन्तता होती है। वहीं, न्याय और वैशेषिक दर्शनों में आत्मा को अचेतन और बाहरी संपर्क से चेतना प्राप्त करने वाला माना गया है।
सांख्य दर्शन में आत्मा को चैतन्य स्वरूप और त्रिगुणातीत माना गया है, और शंकर ने आत्मा को ‘सच्चिदानन्द’ (सत् + चित् + आनन्द) कहा। शंकर के अनुसार आत्मा न तो ज्ञाता है, न ही ज्ञान का विषय। वे केवल एक आत्मा को सत्य मानते हैं, जबकि अन्य दार्शनिक आत्माओं की अनेकता को स्वीकार करते हैं।
कर्म सिद्धान्त: भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त (Law of Karma)
भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धान्त को तीसरे प्रमुख साम्य के रूप में माना जाता है, जो लगभग सभी भारतीय दर्शन प्रणालियों में पाया जाता है। केवल चार्वाक दर्शन इससे अपवाद है, जबकि वेद-विरोधी और वेदांतिक दर्शन दोनों ही कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। कर्म सिद्धान्त को छह आस्तिक और दो नास्तिक दर्शनों ने अपनाया है।
कर्म सिद्धान्त का अर्थ
कर्म सिद्धान्त का सार यह है कि “जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हम काटते हैं।” यह सिद्धान्त बताता है कि शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इसके अनुसार, जो कर्म हम करते हैं, उनका फल कभी नष्ट नहीं होता। साथ ही, बिना किये हुए कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। यह सिद्धान्त, नैतिकता के क्षेत्र में एक ‘कारण-नियम’ के रूप में कार्य करता है, जैसे भौतिक क्षेत्र में हर वस्तु के अस्तित्व का कारण होता है। कर्म सिद्धान्त के अनुसार, हम अपने कर्मों के परिणामों के जिम्मेदार होते हैं और यह जीवन, पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम होता है, जबकि भविष्य का जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का फल होगा।
कर्म सिद्धान्त का ऐतिहासिक और दार्शनिक आधार
कर्म सिद्धान्त का बीज वेदों में विद्यमान है। वैदिक ऋषियों ने नैतिक व्यवस्था के प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी और उसे ‘ऋत’ के रूप में परिभाषित किया, जिसका अर्थ है ‘जगत की व्यवस्था’, जिसमें नैतिकता भी समाहित थी। उपनिषदों में यह सिद्धान्त कर्मवाद के रूप में विस्तारित हुआ। न्याय और वैशेषिक दर्शन में इसे ‘अदृष्ट’ (जो दृष्टिगोचर नहीं है) के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि मीमांसा दर्शन में इसे ‘अपूर्व’ (अज्ञेय) कहा गया है। मीमांसा का मानना है कि कर्म सिद्धान्त स्वतः संचालित है और इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, जबकि न्याय-वैशेषिक दर्शन में यह ईश्वर के अधीन माना गया है।
कर्म सिद्धान्त और निष्काम कर्म
कर्म सिद्धान्त सभी कर्मों पर लागू नहीं होता। यह केवल उन्हीं कर्मों पर लागू होता है जो राग, द्वेष और वासना से संचालित होते हैं। निष्काम कर्म, जो बिना किसी उद्देश्य या इच्छाओं के किए जाते हैं, कर्म सिद्धान्त से स्वतंत्र होते हैं। इन कर्मों का कोई निश्चित परिणाम नहीं होता, जैसे कि बीज बोने के बावजूद वह फल नहीं देते।
कर्म सिद्धान्त के तीन प्रकार
कर्म शब्द का प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है:
- संचित कर्म: वह कर्म, जिसका परिणाम अभी नहीं आया है, और यह पिछले जीवन के कर्मों से उत्पन्न होता है।
- प्रारब्ध कर्म: वह कर्म जिसका फल वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, और यह पिछले जीवन से संबंधित होता है।
- संचीयमान कर्म: वह कर्म जो वर्तमान जीवन में किए जा रहे हैं, और जिनका परिणाम भविष्य में मिलेगा।
कर्म सिद्धान्त पर आलोचनाएँ
कर्म सिद्धान्त पर कई आलोचनाएँ की गई हैं।
- ईश्वरवाद का विरोध: कुछ आलोचक मानते हैं कि कर्म सिद्धान्त, ईश्वर के गुणों का विरोध करता है, क्योंकि इसके अनुसार ईश्वर किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के फल से वंचित नहीं कर सकता।
- सामाजिक दायित्वों में शिथिलता: यह आलोचना की जाती है कि कर्म सिद्धान्त दूसरों की मदद करने का उत्साह कम करता है, क्योंकि यह मानता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हालांकि, यह आलोचना उन लोगों से आती है जो अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं।
- माम्यवाद (Fatalism): आलोचक यह मानते हैं कि कर्म सिद्धान्त, व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करता है, और सुधार की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन यह निराधार है क्योंकि कर्म सिद्धान्त, मनुष्य को भविष्य में अच्छे कर्म करने का अधिकार प्रदान करता है।
कर्म सिद्धान्त की महत्ता
कर्म सिद्धान्त भारतीय दर्शन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके कई पहलुओं से इसका महत्व स्पष्ट होता है:
- विविधता का कारण: कर्म सिद्धान्त यह स्पष्ट करता है कि संसार में व्यक्तियों के जीवन में जो विषमताएँ हैं, उनका कारण उनके पिछले जीवन के कर्म हैं। हर व्यक्ति समान परिस्थितियों में जन्मता है, फिर भी उनकी स्थिति अलग-अलग होती है। कर्म सिद्धान्त इस विषमता को समझाने में मदद करता है।
- व्यावहारिकता: कर्म सिद्धान्त का पालन करने से मानव अपने अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों को समझकर अपने जीवन में सुधार कर सकता है। यह सिद्धान्त बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करता है।
- सान्त्वना और आत्मजिम्मेदारी: कर्म सिद्धान्त के अनुसार, हम अपने कर्मों के परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। यह हमें सान्त्वना प्रदान करता है और दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देता है।
- आशा का संचार: कर्म सिद्धान्त यह भी सिखाता है कि हम अपने वर्तमान कर्मों के आधार पर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार, यह आशा और सकारात्मकता का संदेश देता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माता है।
भारतीय दर्शन में आत्मा, मुक्ति और कर्म के सिद्धांत जीवन के गहरे उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आत्मा को शाश्वत और अविनाशी माना गया है, जो ब्रह्म के साथ एकत्व की अवस्था में है। भारतीय दर्शन यह समझाता है कि संसार में दुःखों का कारण अज्ञान और गलत कर्म होते हैं, और इनसे मुक्ति केवल आत्मज्ञान और सही कर्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे जीवन के परिणाम को प्रभावित करते हैं, और इन्हीं कर्मों से हमें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। मोक्ष, या मुक्ति, संसार के बंधनों से छुटकारा और आत्मा का ब्रह्म से मिलन है। इस प्रकार, भारतीय दर्शन हमें जीवन के उद्देश्य को समझने, आत्म-ज्ञान प्राप्त करने और दुःखों से मुक्ति पाने के लिए मार्गदर्शन करता है, जो जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।


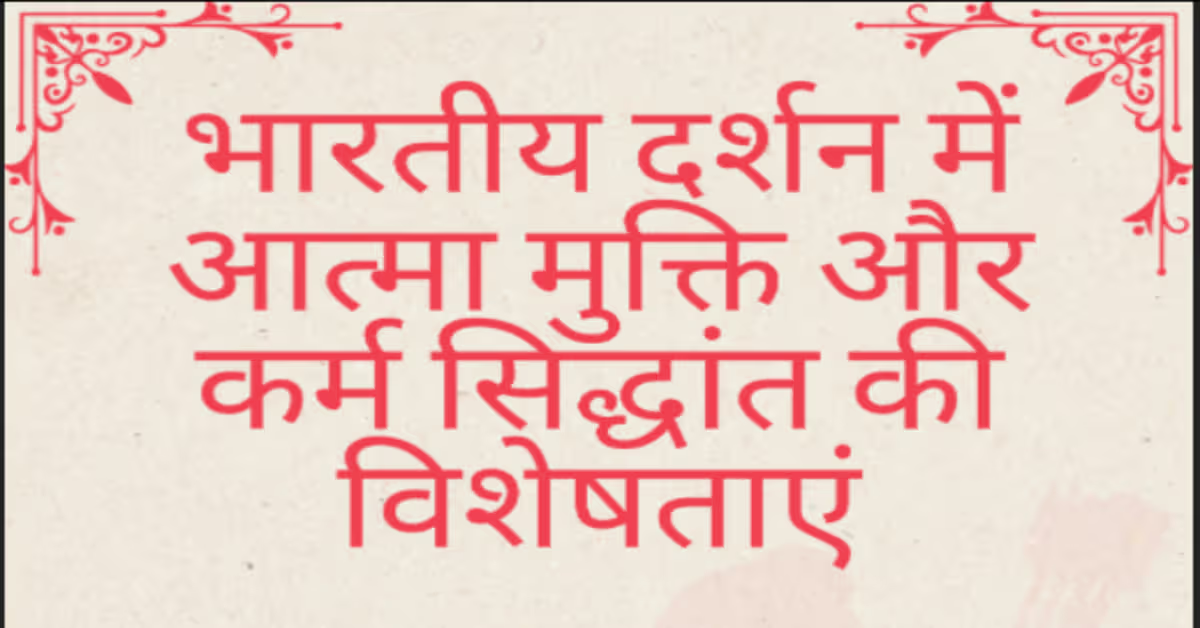
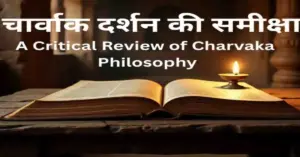

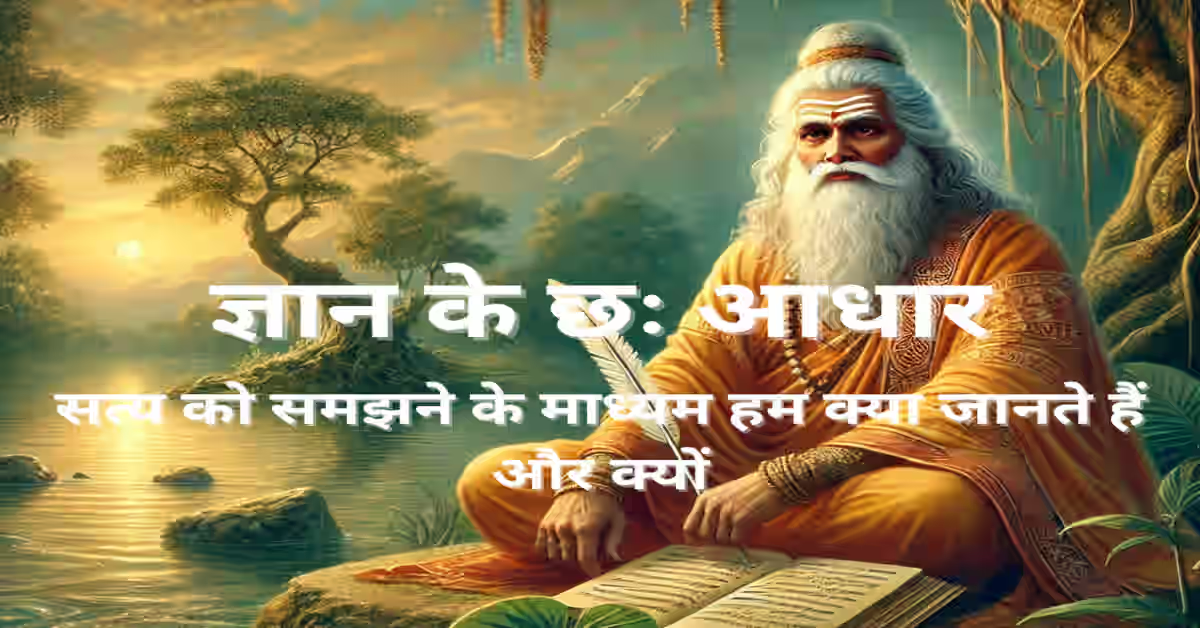
Pingback: भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धान्त और व्यावहारिकता - Shivoham