वेद विश्व-साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। यह मानव-भाषा में प्राचीनतम् मनुष्य के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का सर्वप्रथम परिचय प्रस्तुत करता है। डॉ. राधाकृष्णन ने कहा है, “वेद मानव-मन से प्रादुर्भूत ऐसे नितांत आदि-कालीन प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं।” बिल्सन ने भी इस तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा है, “वेदों से हमें प्राचीनता के संबंध में जो कुछ भी जानने योग्य है, उसकी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है।” यही कारण है कि वेद को अमूल्य निधि के रूप में स्वीकारा गया है।
वेदों के रचयिता को जानने का प्रयास निरर्थक होगा क्योंकि इनके रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं हैं। वेदों में उन सत्य सिद्धांतों का वर्णन है, जिनका दर्शन कुछ मनीषियों को हुआ था। इन्हें देववाणी या श्रुति माना गया है। वेदों को परम सत्य स्वीकारा गया है और इनमें लौकिक और अलौकिक ज्ञान का भंडार भरा हुआ है।
वेद चार हैं:
1. ऋग्वेद:
इसमें उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते थे। कहा जाता है कि आर्य जब अपनी प्राचीन मातृभूमि से भारत आए, तो वे ये मंत्र अपने साथ लाए।
2. यजुर्वेद:
इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यह शुद्ध कर्मकांड संबंधी ग्रंथ है।
3. सामवेद:
यह संगीत प्रधान वेद है। इसमें भी याज्ञिक मंत्रों की प्रधानता है।
4. अथर्ववेद:
इसमें जादू, टोना और मंत्र-तंत्र से संबंधित विधियां हैं। यह भिन्न भावनाओं से ओत-प्रोत है।
चारों वेदों में ऋग्वेद को प्रधान और मौलिक कहा गया है। इसका एक कारण इसका अन्य वेदों से अधिक प्राचीन और व्यापक होना है।
प्रत्येक वेद के तीन मुख्य अंग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्। संहिता में उन मंत्रों का संग्रह होता है जो मुख्यतः सामूहिक पूजा और देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे गए हैं। इसके बाद आने वाले वैदिक साहित्य को ‘ब्राह्मण’ कहा जाता है, जो सामान्यत: गद्य रूप में होते हैं और इनमें यज्ञ की विधियाँ, धार्मिक कार्यों की प्रक्रिया और उनके परिणामों पर विचार किया जाता है। ब्राह्मण के अंत में ‘आरण्यक’ होते हैं, जो विशेषकर वनवासियों के लिए उपासनाओं का वर्णन करते हैं। इसके बाद ‘उपनिषद्’ आते हैं, जो गहरे दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण होते हैं। इन्हें ‘ज्ञानकांड’ भी कहा जाता है और यह वेद के अंतिम अंग माने जाते हैं, जिन्हें ‘वेदांत‘ भी कहा जाता है
वेदों के अध्ययन की आवश्यकता
वेदों का अध्ययन अत्यंत लाभप्रद है। आज के वैज्ञानिक युग में भी यह आवश्यक है।
- ज्ञान का स्रोत: वेद लौकिक और अलौकिक दोनों विषयों का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह ज्ञान-विज्ञान के भंडार हैं।
- इतिहास को समझने का माध्यम: वेदों के अध्ययन के बिना भारत के धार्मिक और दार्शनिक इतिहास को समझ पाना असंभव है।
- हिंदू धर्म की विशेषताएं: वेदों में हिंदू धर्म की अनेक विशेषताएं निहित हैं। इस धर्म के विशेष ज्ञान के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है।
- आदिम मनुष्य का परिचय: वेद हमें आदिम मनुष्य की मानसिक स्थिति और जीवनशैली के बारे में भी गहन जानकारी प्रदान करते हैं।
दार्शनिक प्रवृत्तियां
ऋग्वेद में कवि हृदयों के उद्गार झलकते हैं। वैदिक ऋषि जगत और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे।
- जगत का स्वरूप: वैदिक ऋषियों ने जगत के स्वरूप को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया।
- देवताओं पर शंका: वे पूजित देवताओं के विषय में भी प्रश्न करने लगे। यही प्रवृत्तियां दार्शनिक विचारों की शुरुआत थीं, जिनका पूर्ण विकास उपनिषदों में हुआ।
- ज्ञान और सुख की खोज: वेदों का परम ध्येय ज्ञान और सुख की प्राप्ति है। वैदिक ऋषि प्रकृति के रहस्यों को समझने के साथ-साथ परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे।
ऋषि संसार के दुःखों से परिचित थे। सांसारिक दुःखों से मुक्ति पाने की अभिलाषा उनके मन में स्पष्ट दिखाई देती है।
- मृत्यु का भय: मृत्यु के भय से प्रेरित होकर ऋषि दीर्घ जीवन और परम सुख की प्रार्थना करते हैं।
- जीवात्मा और परमात्मा का एक्य: वेदों के अनुसार, जीवात्मा और परमात्मा के एक्य से ही शांति और सुख की प्राप्ति संभव है। यही वेदों का अंतिम और परम लक्ष्य है।
जगत् - विचार
वेद-दर्शन में जगत् को सत्य और पूर्ण रूप से व्यवस्थित माना गया है। हालांकि देवताओं की संख्या अनेक बताई गई है, फिर भी वह संसार, जिस पर वे शासन करते हैं, एक ही है। जहां तक विश्व की उत्पत्ति का प्रश्न है, वेद-दर्शन में विभिन्न विचार पाए जाते हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में न ‘सत्’ था, न ‘असत्’, न ‘आकाश’ था, न ‘अन्तरिक्ष’, और न ही मृत्यु थी। केवल एक ‘वह’ था, और सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था। जल था, किंतु प्रकाश नहीं था। तब ‘तपस्’ से उस एक की उत्पत्ति हुई, जो एक अव्यक्त चेतना थी, और इसी से सृष्टि की रचना हुई। तपस् से ज्ञानशक्ति, इच्छा और क्रिया शक्ति का उदय हुआ। वेद के अन्य मंत्रों में अग्नि से जगत् की उत्पत्ति मानी गई है, जबकि कुछ अन्य मतों में सोम से पृथ्वी, आकाश, दिन, रात, जल आदि की उत्पत्ति की बात कही गई है। इस प्रकार, विश्व की उत्पत्ति के संबंध में वेदों में विविध दृष्टिकोण मिलते हैं।
नीति और धर्म
वेदों को दो खंडों में विभाजित किया गया है: (1) ज्ञानकांड और (2) कर्मकांड।
ज्ञानकांड में आध्यात्मिक चिंतन है, जबकि कर्मकांड में उपासना और यज्ञ का महत्व बताया गया है। कर्मकांड में अधिकार भेद का उल्लेख मिलता है। सभी कर्मों को हर व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। अधिकार के बिना कर्म करने से बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और प्रयत्न विफल हो जाते हैं। वेदों में अधिकार के अनुसार कर्म करने का निर्देश दिया गया है।
वेदों में तपस्या, स्तुतियां, पवित्र विचार, और अंतःकरण की शुद्धि को परम तत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। ‘ऋत’ का विचार वेदों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऋत नैतिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। देवताओं को नैतिक नियमों का पालन करने और करवाने वाला माना गया है। ‘ऋत’ का अर्थ है जगत् की व्यवस्था, जिसे प्राकृतिक नियम (Natural Law) कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन, और रात जैसे सभी घटनाएं इसी नियम से संचालित होती हैं। यह नियम देवताओं पर भी लागू होता है। ‘ऋत’ समस्त जगत का आधार है।
जगत् का संचालन ‘वरुण’ देवता द्वारा किया जाता है। स्वर्ग और नरक, दोनों ही वर्तमान स्थिति में ‘ऋत’ के कारण हैं। ‘ऋत’ के सिद्धांत में कर्म सिद्धांत (Law of Karma) का बीज निहित है, जो आगे चलकर पुनर्जन्म के विचार की ओर संकेत करता है।
वेदों में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है, परंतु मृत्यु के उपरांत के जीवन के बारे में वेद अस्पष्ट हैं। वैदिक आर्यों को अपने जीवन से प्रेम था, क्योंकि उनका जीवन आनंदमय और सबल था। इसलिए, पुनर्जन्म के विचार की उन्हें विशेष आवश्यकता नहीं महसूस हुई।
स्वर्ग और नरक के संदर्भ में वेदों में अस्पष्ट विचार मिलते हैं। स्वर्ग के सुखों को पृथ्वी के सुखों से अधिक माना गया है। स्वर्ग में अमरता की प्राप्ति होती है। नरक को अंधकारमय कहा गया है। वरुण पापियों को नरक में भेजते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक का अधिकारी बनता है।
धर्म का स्वरूप
वेदों में बहुदेववाद (Polytheism) का विचार प्रमुख है। अनेक देवताओं को उपासना का विषय माना गया है, जैसे इंद्र, वरुण, सोम, चंद्रमा, यम, सविता, पूषन, और अग्नि। इन देवताओं की स्तुतियों की रचना की गई है।
वैदिक देवताओं का व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं है। ब्लूमफील्ड के अनुसार, वैदिक देवता मनुष्य के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक देवताओं का मानवीकरण हुआ है। वे हाथ, पांव आदि मनुष्यों की तरह रखते हैं, युद्ध करते हैं, भोज में भाग लेते हैं, मद्यपान करते हैं, और दानवों से संघर्ष करते हैं।
वैदिक धर्म में प्रार्थना को विशेष महत्व दिया गया है। प्रार्थना के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। वैदिक धर्म जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस धर्म में मूर्तिपूजा का उल्लेख नहीं मिलता। उस समय देवताओं के मंदिर नहीं थे। वेदों में मानव और ईश्वर के बीच सीधा संबंध दिखता है। देवताओं को मनुष्य का मित्र माना गया है।
वैदिक देवता
ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए हैं। इन मंत्रों में विभिन्न देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इससे प्रमाणित होता है कि वेद में अनेक देवताओं के विचार समाहित हैं। इन देवताओं को प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का स्वामी कहा गया है। वे एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे प्राकृतिक शक्तियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, वैसे ही वैदिक देवता भी आपस में जुड़े हुए हैं।
वैदिक काल के देवताओं का कोई स्पष्ट और स्थायी व्यक्तित्व नहीं था। वे ग्रीक देवताओं की तरह निश्चित नहीं थे। देवताओं की संख्या अधिक होने का कारण यह था कि वैदिक ऋषि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अपने सरल हृदय से आनंदित हो जाते थे और उन दृश्यों को देवताओं का रूप दे देते थे। इस प्रकार, प्राकृतिक वस्तुओं में देव-भाव का आरोपण किया गया, जिससे देवताओं की संख्या बढ़ गई।
‘देव’ का अर्थ है, जो अपनी गरिमा से चमकते हैं। वैदिक काल के देवताओं को ‘देव’ इसलिए कहा गया क्योंकि वे समस्त सृष्टि को प्रकाश देते हैं और अपनी गरिमा से चमकते रहते हैं।
वैदिक देवताओं का परिचय
वरुण: वैदिक युग का सबसे प्रसिद्ध देवता वरुण है, जो आकाश का देवता है। ‘वरुण’ शब्द ‘वर’ धातु से निकला है, जिसका अर्थ है ढकना। वरुण को समस्त पृथ्वी को आच्छादित करने वाला माना गया है। वह शांति प्रिय देवता, प्राकृतिक और नैतिक नियमों का संरक्षक और सर्वज्ञ है। वरुण को ऋत (सार्वभौमिक नियम) का रक्षक कहा गया है। वह पापियों को दंड देता है और पश्चाताप करने वालों को क्षमा करता है।
मित्र: मित्र देवता वरुण के सहचारी हैं। वह सूर्य और प्रकाश के प्रतीक हैं। उनकी प्रार्थना वरुण के साथ की जाती है।
इंद्र: इंद्र का स्थान वैदिक देवताओं में प्रमुख है। उन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना गया है। वह वज्र धारण करते हैं और अंधकार पर विजय पाते हैं। इंद्र को भारतीय ज़्यूस (Zeus) कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए की गई है।
वायु (वात): वायु देवता को सर्वत्र व्याप्त माना गया है। उनका शब्द सुनाई देता है लेकिन वह दिखाई नहीं देते।
मरुद्गण और रुद्र: मरुद्गण तुफानों के देवता हैं, और रुद्र को भयंकर आवाज़ करने वाला देवता कहा गया है।
यम: यम को मृत्यु का देवता माना गया है।
सोम: सोम को प्रेरणा और अमरत्व का देवता माना गया है। वह मादकता का प्रतीक हैं।
विष्णु: विष्णु सौर मंडल के देवता हैं। उनकी तीन विशेषताएँ हैं—वे पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में विचरण करते हैं।
सूर्य और सविता: सूर्य को प्रकाश और कर्म में प्रवृत्त करने वाला देवता माना गया है। सविता सूर्य देवता का ही एक रूप हैं।
उषा: उषा प्रभात की देवी और रात्री की बहन हैं। वह स्वर्ग का द्वार खोलती हैं।
अग्नि: अग्नि का स्थान भी प्रमुख है। वह यज्ञ के देवता हैं और देवताओं तक हवि पहुँचाते हैं। अग्नि को ऋग्वेद में 200 से अधिक मंत्रों में संबोधित किया गया है।
पोषण: पोषण को चारागाह और पशुओं का संरक्षक माना गया है।
वैदिक धर्म का विकास
वेदों में अनेक देवताओं का वर्णन है। यह विचार अनेकेश्वरवाद (Polytheism) की ओर संकेत करता है। अनेकेश्वरवाद का अर्थ है अनेक देवताओं में विश्वास।
लेकिन धार्मिक चेतना ने केवल अनेकेश्वरवाद को स्वीकार नहीं किया। वैदिक ऋषियों के सामने यह प्रश्न था कि इन देवताओं में किसे श्रेष्ठ मानकर आराधना की जाए। इस विचार से एक प्रवृत्ति विकसित हुई जिसमें एक देवता को सर्वोच्च माना गया। इसे हीनोथीज्म (Henotheism) कहा गया। इस प्रवृत्ति में उपासना के समय एक देवता को सबसे बड़ा माना जाता था। जैसे, जब अग्नि की पूजा होती, तो उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था।
डॉ. राधाकृष्णन ने हीनोथीज्म को धर्म का स्वाभाविक निष्कर्ष बताया है। शनैः-शनैः हीनोथीज्म का संक्रमण एकेश्वरवाद (Monotheism) में हुआ। वैदिक ऋषि प्रकृति की एकता और व्यवस्था को देखकर सभी देवताओं को एक ही शक्ति का रूप मानने लगे।
एकेश्वरवाद का संकेत
ऋग्वेद में एकेश्वरवाद के संकेत मिलते हैं। एक मंत्र कहता है:
“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।”
अर्थात, सत्य एक है, विद्वान उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं—कोई अग्नि, कोई यम और कोई मातरिश्वा।
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वैदिक धर्म का विकास अनेकेश्वरवाद से होकर हीनोथीज्म और फिर एकेश्वरवाद की ओर हुआ। यह विकास वैदिक धर्म की धार्मिक चेतना और प्रकृति की एकता को दर्शाता है।


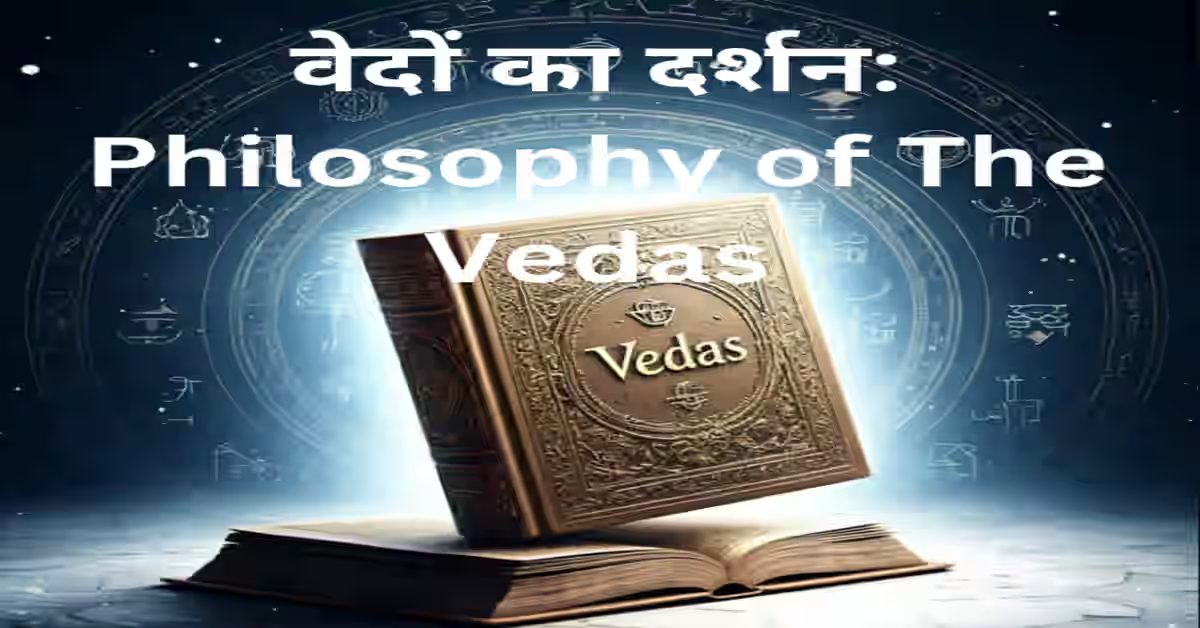
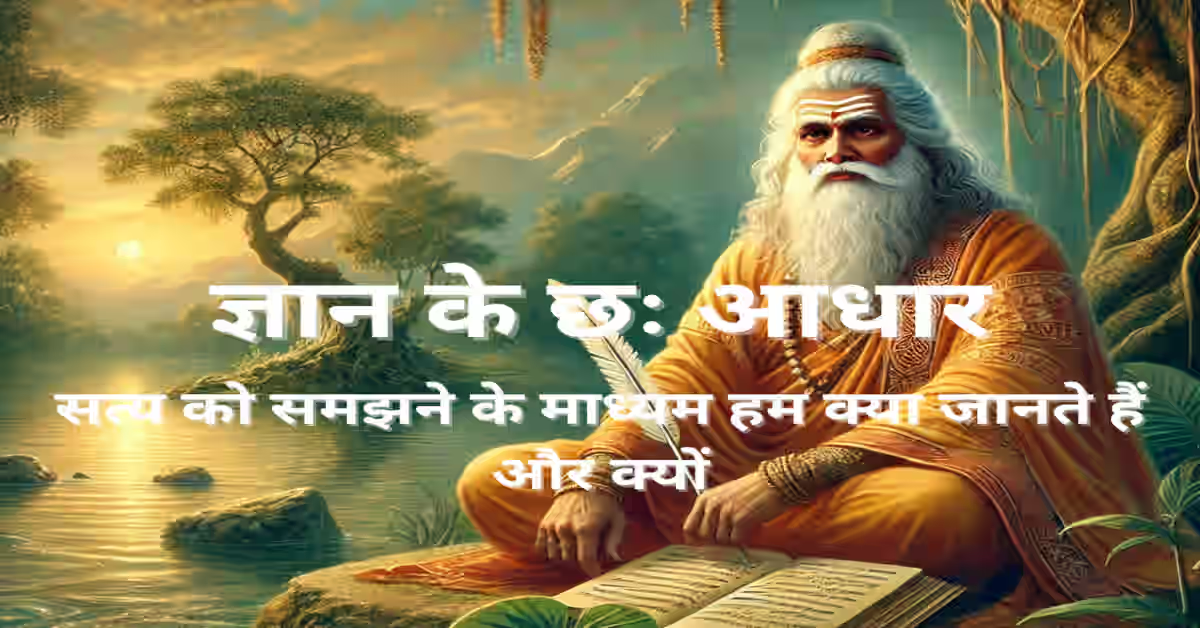
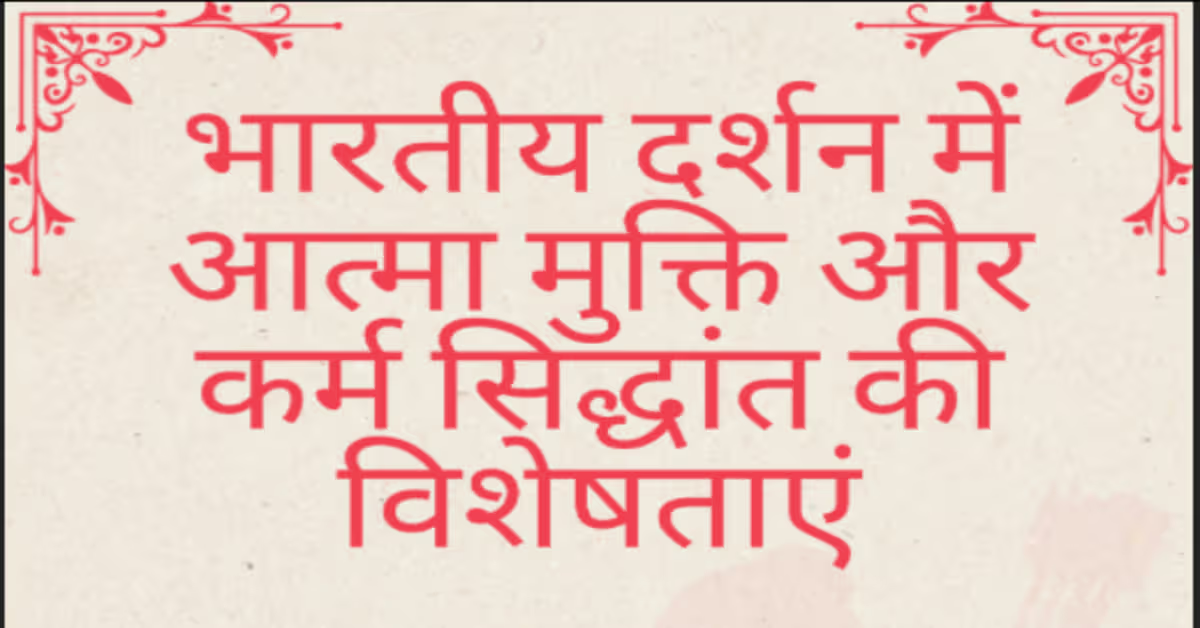
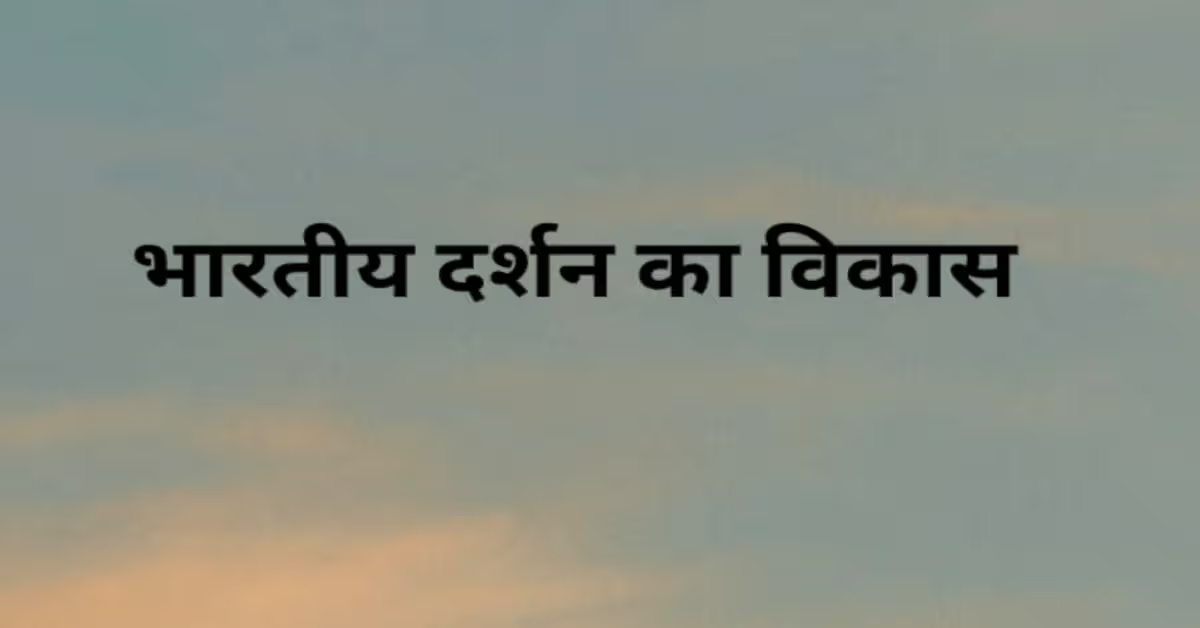
Pingback: उपनिषदों का दर्शन (Philosophy Of The Upanisads) - Shivoham