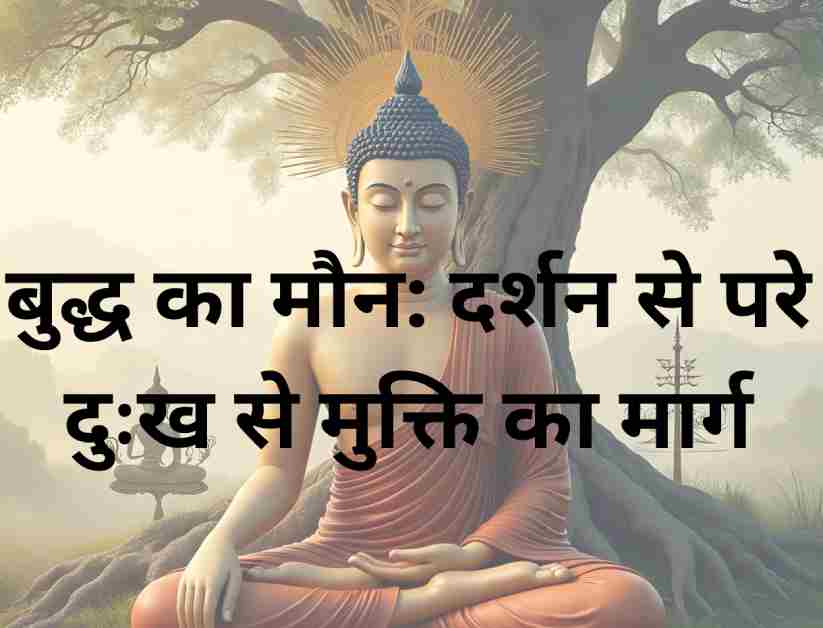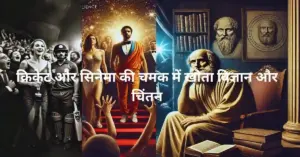बुद्ध की तत्त्व-शास्त्र के प्रति विरोधात्मक प्रवृत्ति (Anti-metaphysical attitude of Buddha)
प्रत्येक दार्शनिक, कवि की ही भाँति, अपने समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। बुद्ध का जन्म जिस समय हुआ था, उस समय मानव समाज तत्त्वशास्त्र की समस्याओं को सुलझाने में अत्यधिक व्यस्त था। हर व्यक्ति आत्मा, जगत और ईश्वर जैसे विषयों के चिंतन में डूबा रहता था। जितने विचारक थे, उतने ही मत प्रचलित हो गए थे। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि लोगों का नैतिक जीवन शिथिल होने लगा था। वे अपने जीवन के कर्तव्यों को भूलते जा रहे थे। संसार में रहते हुए भी वे संसार से कोसों दूर प्रतीत होते थे। नीति-शास्त्र के नियमों के प्रति उनकी आस्था डगमगा गई थी। जिस प्रकार विचार-क्षेत्र में अराजकता व्याप्त थी, उसी प्रकार नैतिक-क्षेत्र में भी अव्यवस्था थी। ऐसे समय समाज को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो उन्हें नैतिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाए। बुद्ध इस आवश्यकता की पूर्ति करने में पूर्णत: सफल हुए।
बुद्ध मूल रूप से एक समाज-सुधारक थे, दार्शनिक नहीं। दार्शनिक उस व्यक्ति को कहा जाता है, जो ईश्वर, आत्मा और जगत जैसे विषयों का चिंतन करता है। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं का अवलोकन करते हैं तो वहाँ हमें आचार-शास्त्र, मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र तो मिलते हैं, लेकिन तत्त्व-दर्शन का पूर्णत: अभाव दिखाई देता है। जब भी उनसे दर्शन-शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता था, वे मौन साध लेते थे। आत्मा और जगत से संबंधित कई लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति उन्होंने सदैव मौन रहकर उदासीनता का परिचय दिया।
इन प्रश्नों को पाली साहित्य में अव्याकरणि (Indeterminable Questions) कहा गया है। ऐसे दस प्रश्न इस प्रकार हैं—
क्या यह विश्व शाश्वत (Eternal) है?
क्या यह विश्व अशाश्वत (Non-eternal) है?
क्या यह विश्व सीमित (Finite) है?
क्या यह विश्व असीम (Infinite) है?
क्या आत्मा और शरीर एक ही हैं?
क्या आत्मा शरीर से भिन्न है?
क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है?
क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म नहीं होता है?
क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना — दोनों बातें सत्य हैं?
क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना — दोनों बातें असत्य हैं?
इन दस प्रश्नों में प्रथम चार विश्व से संबंधित हैं, अगले दो आत्मा से और अंतिम चार तथागत से। बौद्ध दर्शन में तथागत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। इन प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध का मौन रहना सदैव चर्चा का विषय रहा है और इसके अनेक अर्थ लगाए गए हैं।
कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध इन तत्त्वशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे, इसलिए वे मौन रहते थे। उनके अनुसार बुद्ध का मौन रहना उनके अज्ञान का प्रतीक है।
लेकिन बुद्ध के मौन को अज्ञान कहना उनके साथ अन्याय होगा। यदि वे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते, तो वे स्वयं को बुद्ध (अर्थात् ज्ञानी – Enlightened) कहलवाते ही क्यों? वास्तव में, “बुद्ध” का अर्थ ही ज्ञानी है। इस दृष्टि से बुद्ध को अज्ञानी कहना, उनके नाम और उपाधि को ही निरर्थक बना देना है।
बुद्ध की तत्त्व-शास्त्र के प्रति मौन प्रवृत्ति का अर्थ
कुछ विद्वानों का मत है कि बुद्ध आत्मा, जगत और ईश्वर जैसे विषयों के अस्तित्व को लेकर संशय करते थे। उनके अनुसार बुद्ध का मौन रहना उनके संशयवाद की स्वीकृति है। लेकिन यह अर्थ उचित नहीं है। यदि बुद्ध संशयवादी होते, तो वे स्वयं को बुद्ध (ज्ञानी) नहीं कहते। उनका पूरा दर्शन इस बात का प्रमाण है कि वे संशयवाद के समर्थक नहीं थे।
अनेक आचार्यों ने बुद्ध के मौन का दूसरा अर्थ निकाला है। उनका मानना है कि बुद्ध का मौन रहना एक निश्चित उद्देश्य को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्ध जानबूझकर तत्त्वशास्त्रीय प्रश्नों पर मौन रहते थे। वे सर्वज्ञानी थे और मानव ज्ञान की सीमाओं को भली-भांति जानते थे। उन्होंने देखा कि तत्त्वशास्त्र से जुड़े प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिए जा सकते। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर दार्शनिकों में मतभेद रहा है। ऐसे में इन प्रश्नों पर चर्चा करना केवल व्यर्थ के विवाद को जन्म देना है।
बुद्ध ने अंधों और हाथी की उपमा देकर इस तथ्य को समझाया। जैसे अंधे लोग हाथी को छूकर अलग-अलग वर्णन करते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते, वैसे ही मनुष्य आत्मा, ईश्वर और जगत जैसे विषयों का पूर्ण ज्ञान पाने में असमर्थ है। इसलिए बुद्ध के अनुसार तत्त्वशास्त्रीय प्रश्नों में उलझना बुद्धिमानी नहीं है।
इसके अतिरिक्त बुद्ध इस कारण भी मौन रहते थे कि वे जानते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर व्यावहारिक दृष्टि से कोई उपयोगी परिणाम नहीं देता। उनके अनुसार संसार दुःखों से भरा हुआ है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दुःख और उसके निवारण को जाने। उन्होंने दर्शन का वास्तविक उद्देश्य “दुःख का अन्त” (Cessation of suffering) बताया। स्वयं बुद्ध ने कहा है—
“मैं केवल दुःख और दुःख-निरोध पर ही अधिक जोर देता हूँ।”
उन्होंने एक सुंदर उपमा द्वारा इसे स्पष्ट किया। यदि कोई व्यक्ति बाण से घायल होकर किसी के पास पहुँचे, तो उसका पहला कर्तव्य होगा कि बाण को निकालकर घाव का उपचार किया जाए। यदि वह इसके बजाय यह सोचने लगे कि बाण कैसा है, किसने मारा, कहाँ से मारा और तीर मारने वाले का रंग-रूप क्या था—तो यह मूर्खता होगी। उसी प्रकार दुःख से पीड़ित मानव के लिए आत्मा, ईश्वर और जगत जैसे प्रश्नों में उलझना व्यर्थ है। इसलिए तत्त्वशास्त्र संबंधी प्रश्नों पर बुद्ध का मौन रहना एक प्रयोजनात्मक मौन था। यही इस मौन का सही अर्थ है।
निष्कर्ष: मौन में जो कहा नहीं गया, वह भी कहा गया
बुद्ध का मौन कोई निष्क्रियता नहीं थी। वह एक सशक्त प्रतिरोध था — उस जटिल दर्शन के विरुद्ध, जिसने मनुष्य को वास्तविक समस्याओं से विमुख कर दिया था। उनकी दृष्टि में सच्चा दर्शन वही है जो दुःख को समाप्त करे। उन्होंने कहा नहीं, पर बहुत कुछ कह दिया — अपने मौन से।
बुद्ध का यह मौन हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में छिपे होते हैं।