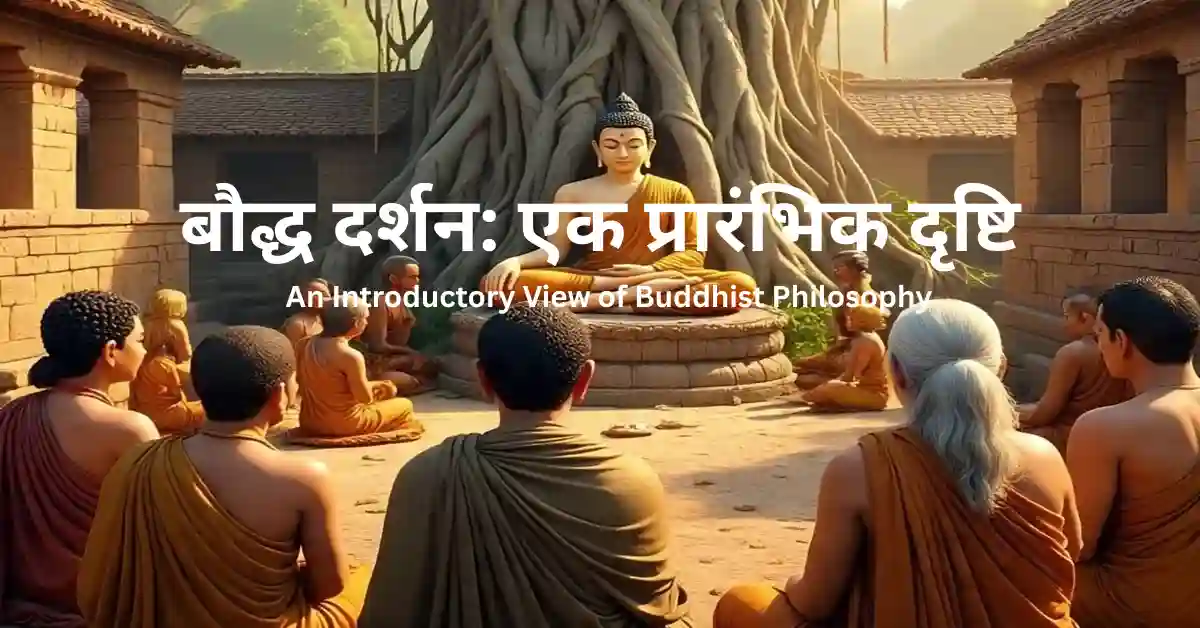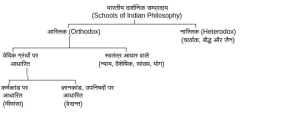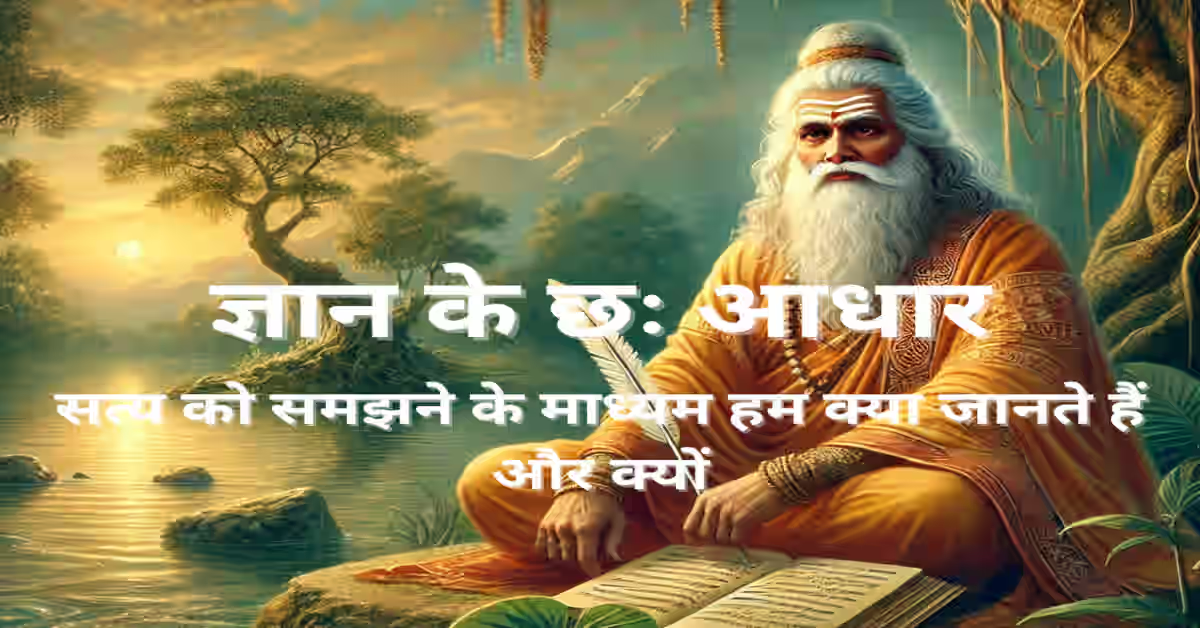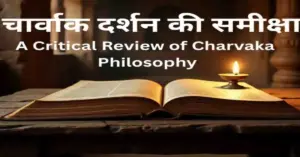बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। उनका जन्म ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य राजवंश में हुआ था। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया।
राजकुमार होने के कारण उनके पिता ने यह प्रयास किया कि सिद्धार्थ का जीवन केवल सुख-सुविधाओं में बीते और उनका मन कभी भी संसार की क्षणभंगुरता और दुख की ओर न जाए। इसके लिए महल में हर प्रकार के मनोरंजन और विलास की व्यवस्था की गई। लेकिन इन सभी प्रयत्नों के बावजूद सिद्धार्थ का मन संसार की दुखभरी वास्तविकताओं से बच न सका।
कहा जाता है कि एक दिन जब वे नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने तीन दृश्य देखे—एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध और एक शव जिसे श्मशान ले जाया जा रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के संवेदनशील हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। तभी उन्हें यह अनुभव हुआ कि संसार का स्वभाव दुखमय है। यह विचार उन्हें लगातार व्याकुल करता रहा कि दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है।
इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक रात वे अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर महल से निकल पड़े और संन्यास ग्रहण कर लिया। पत्नी का स्नेह, पुत्र का मोह और महल का वैभव भी सिद्धार्थ को सांसारिक बंधनों में नहीं रोक पाया।
लंबे समय तक कठिन साधना और तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान (बोधि) प्राप्त हुआ। सत्य का बोध होने के बाद वे बुद्ध (अर्थात् “जाग्रत” या “ज्ञानी”) कहलाए। इसके अलावा उन्हें तथागत (यानी “वह जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान चुका हो”) और अर्हत (The Worthy) की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने लोककल्याण के उद्देश्य से अपने उपदेश जनता तक पहुँचाने का निश्चय किया। वे गाँव-गाँव घूमकर लोगों को समझाने लगे कि दुख क्यों है और दुख से मुक्ति का उपाय क्या है। बुद्ध के इन उपदेशों से आगे चलकर बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का विकास हुआ।
प्रारंभ में बौद्ध धर्म भारत में ही फैला। इसका मुख्य कारण था—उस समय के प्रचलित धर्म से लोगों की असंतुष्टि। उस काल में ब्राह्मण धर्म का प्रभुत्व था, जिसमें बलि प्रथा आम थी। लोग पशु ही नहीं, बल्कि कभी-कभी मनुष्य तक की बलि चढ़ाने में संकोच नहीं करते थे। हिंसा से भरे इस वातावरण में बुद्ध का धर्म, जो अहिंसा और करुणा पर आधारित था, जनता के बीच शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया।
कुछ ही समय बाद यह धर्म भारत की सीमाओं से बाहर भी फैल गया। राजाओं और भिक्षुओं की सहायता से यह कई देशों तक पहुँचा और धीरे-धीरे एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित हो गया।
बौद्ध दर्शन की शाखाएँ
बौद्ध दर्शन के बहुत से अनुयायी हुए। समय के साथ अनुयायियों में मतभेद पैदा हुए और बौद्ध दर्शन की कई शाखाएँ बन गईं। इन शाखाओं से उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन का विकास हुआ, जिसमें दार्शनिक विचारों की प्रधानता थी। यह उत्तरकालीन रूप कई मामलों में प्रारंभिक बौद्ध दर्शन से भिन्न और कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत होता है।
हालाँकि, यहाँ हम उत्तरकालीन विचारों के बजाय केवल प्रारंभिक बौद्ध दर्शन का अध्ययन करेंगे, जो स्वयं बुद्ध के व्यक्तिगत विचारों और उपदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
त्रिपिटक : बौद्ध दर्शन का आधार
बुद्ध ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके उपदेश मौखिक रूप से दिए जाते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इन उपदेशों को संकलित कर त्रिपिटक नामक ग्रंथ तैयार किया।
“त्रिपिटक” शब्द का अर्थ है तीन पिटारियाँ (त्रि = तीन, पिटक = पिटारी/Box)। वास्तव में यह तीन पिटारियाँ ही बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह हैं—
सुत्त पिटक – इसमें धर्म और उपदेशों का वर्णन है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद इसी का हिस्सा है।
अभिधम्म पिटक – इसमें बुद्ध के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचार संकलित हैं।
विनय पिटक – इसमें नैतिक नियम और भिक्षुओं के आचार-व्यवहार का वर्णन है।
त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई और माना जाता है कि इसका संकलन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसे प्रारंभिक बौद्ध दर्शन का सबसे प्रामाणिक आधार माना जाता है।
त्रिपिटक के अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है—मिलिंद पन्हो (मिलिंद-प्रश्न)। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद के बीच हुए संवाद का वर्णन है। प्रसिद्ध विद्वान रीज डेविड्स (Rhys Davids) ने इस ग्रंथ की साहित्यिक दृष्टि से बहुत प्रशंसा की है। बाद में बुद्धघोष ने भी इसे त्रिपिटक के बाद बौद्ध दर्शन का एक प्रामाणिक और प्रशंसनीय ग्रंथ माना।
बुद्ध की मुख्य शिक्षाएँ
बुद्ध की सबसे प्रमुख शिक्षा है चार आर्य सत्य (The Four Noble Truths)। लेकिन इन्हें समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि बुद्ध का तत्त्वज्ञान (Metaphysics) के प्रति क्या दृष्टिकोण था।
इसलिए अब हम आगे बुद्ध की तत्त्वशास्त्र के प्रति सोच और रुख पर प्रकाश डालेंगे।