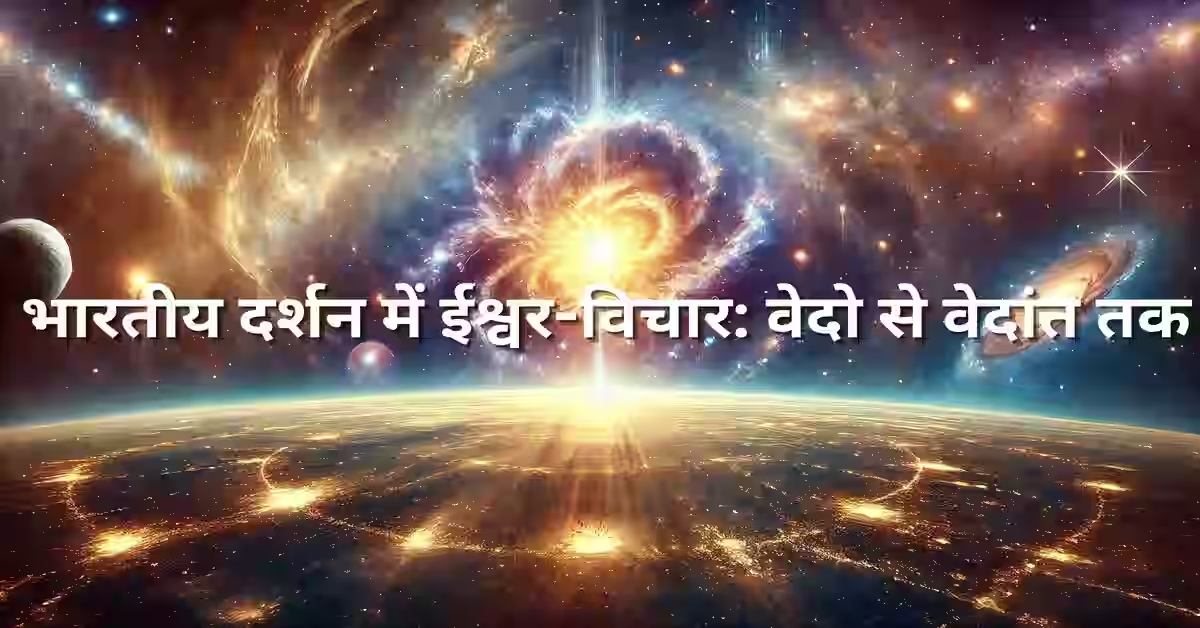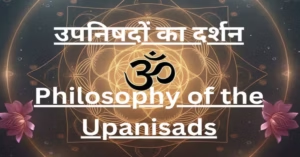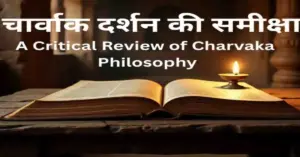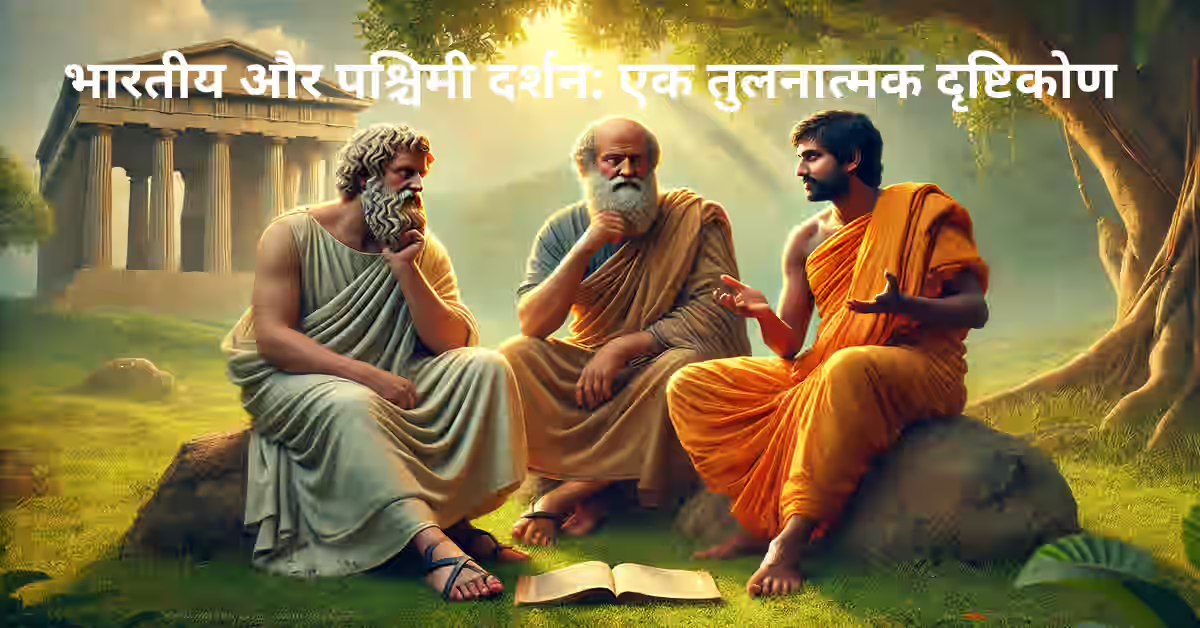भारतीय दर्शन में ईश्वर-विचार का मूल स्रोत वेद, विशेष रूप से ऋग्वेद, को माना जाता है। ऋग्वेद में ही भारतीय दर्शन के अधिकांश सिद्धांत बीज रूप में निहित हैं, जिनमें ईश्वर से संबंधित विचार भी शामिल हैं। इन विचारों का उद्घाटन वैदिक ग्रंथों से लेकर आधुनिक भारतीय दार्शनिकों तक विभिन्न रूपों में किया गया है। इस प्रकार, भारतीय दर्शन में ईश्वर-संबंधी सभी प्रमुख विचार वेदों में प्रकट होते हैं और उनसे प्रेरित होकर आगे के दार्शनिक विचार विकसित हुए हैं।
वैदिक मत
भारतीय दर्शन में ईश्वर संबंधी सभी प्रमुख विचार वेदों में बीज रूप में निहित हैं। इनमें अनेकेश्वरवाद (Polytheism), प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद (Naturalistic Polytheism), संगठित अनेकेश्वरवाद (Organized Polytheism), हेनोथिज्म (Henotheism), त्रयेश्वरवाद (Tritheism), एकेश्वरवाद (Monotheism) आदि सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है।
(क) अनेकेश्वरवाद (Polytheism)
वैदिक ऋषि अनेक देवी-देवताओं में विश्वास रखते थे। वेदों में अनेक देवताओं की कल्पना की गई है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि। वैदिक अनेकेश्वरवाद को प्राकृतिक अनेकेश्वरवाद भी कहा गया, जिसमें प्रकृति की शक्तियों को देवता माना गया।
(ख) हेनोथिज्म (Henotheism)
मैक्समूलर के अनुसार, वैदिक काल में जब किसी देवता की पूजा होती थी, तो उसे ही सर्वोपरि मान लिया जाता था। उदाहरणस्वरूप, अग्नि की पूजा के समय उसे सभी देवताओं से श्रेष्ठ माना जाता था।
(ग) त्रयेश्वरवाद (Tritheism)
त्रयेश्वरवाद के अनुसार, सभी देवताओं को तीन प्रमुख देवताओं – पृथ्वी देवता, आकाश देवता, और वायु देवता – के रूप में देखा गया।
(घ) एकेश्वरवाद (Monotheism)
वैदिक साहित्य में ‘पुरुषसूक्त’ के माध्यम से एकेश्वरवादी विचार प्रकट होते हैं। ईश्वर को परम सत्य और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त तथा उससे परे दोनों माना गया।
ईश्वर का भारतीय दर्शन में स्थान और विभिन्न विचारधाराएँ
ईश्वर भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसका कारण है भारतीय दर्शन पर धर्म की गहरी छाप। धर्म, सामान्यत: ईश्वर में विश्वास को ही संदर्भित करता है, और क्योंकि भारतीय दर्शन धर्म से प्रभावित है, इसलिए ईश्वर के संबंध में यहां व्यापक चर्चा मिलती है। भारतीय विचारधारा में ईश्वर के अस्तित्व और स्वरूप पर विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं, और ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कई तर्कों का उपयोग किया गया है। इसलिए, भारतीय दर्शन में ईश्वर से संबंधित विचारों की विवेचना महत्वपूर्ण है।
भारतीय दर्शन का प्रारंभ बिंदु वेद है, और इसलिए ईश्वर से संबंधित विचारों की शुरुआत वेदों से की जानी चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल के ऋषियों ने अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, उषा, पृथ्वी, मरुत, वायु, वरुण, इन्द्र, सोम आदि देवताओं की पूजा की। इन देवताओं की उपासना के लिए गीतों की रचना की गई थी। वैदिक देवताओं का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं था; इनकी उपासना में अनेकेश्वरवाद की प्रवृत्ति प्रकट होती है, अर्थात, विभिन्न देवताओं में विश्वास किया गया, लेकिन यह विश्वास इस बात को लेकर नहीं था कि हर देवता का स्वतंत्र अस्तित्व है। इस प्रकार, वेदों में अनेकेश्वरवाद के उदाहरण मिलते हैं।
अनेकेश्वरवाद से एकेश्वरवाद की ओर
अनेकेश्वरवाद का मतलब है कि विभिन्न देवताओं में विश्वास किया जाता है, लेकिन यह स्थायी धर्म नहीं बन पाता। वेदों के समय में, इस सवाल ने जन्म लिया कि इन देवताओं में से किसे सर्वोत्तम मानकर पूजा जाए। धार्मिक चेतना ने एक ही देवता को श्रेष्ठ मानने की आवश्यकता को महसूस किया, जिससे एकेश्वरवाद (Monotheism) का उदय हुआ। इस अवधारणा के अनुसार, विभिन्न देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं।
उपनिषदों का ईश्वर-विचार
वेदों के बाद उपनिषदों में ईश्वर का स्थान अपेक्षाकृत गौण प्रतीत होता है। यहां ब्रह्म को चरम तत्व के रूप में स्वीकारा गया है। वेदों में विभिन्न देवता अब पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, और ब्रह्म तथा आत्मा का महत्व बढ़ जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म को अद्वितीय, निराकार और असीम माना गया है, और देवताओं को ब्रह्म का प्रकाशित रूप माना गया है। उपनिषदों में ईश्वर की वास्तविकता पर भिन्न-भिन्न विचार दिए गए हैं, और यह दर्शाया गया है कि ईश्वर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, “यह आत्मा ही ब्रह्म है।” इसे ‘सच्चिदानंद’ (सत्, चित्, आनंद) के रूप में वर्णित किया गया है।
उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन मिलता है: (1) पर-ब्रह्म और (2) अपर-ब्रह्म। पर-ब्रह्म को निराकार और निर्गुण माना गया है, जबकि अपर-ब्रह्म सगुण और साकार है। इन दोनों के बीच का अंतर उपनिषदों के विचार में महत्वपूर्ण है।
भगवद गीता में ईश्वर का स्वरूप
उपनिषदों के बाद, भगवद गीता में ईश्वर के विचार में और विस्तार हुआ है। गीता में ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद का एक साथ समन्वय है। गीता के ‘विश्व रूप दर्शन’ के अध्याय में भगवान के सर्वव्यापी रूप को दर्शाया गया है। गीता में ईश्वर को जगत का परम कारण और नायक माना गया है। गीता के अनुसार, ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण होते हुए भी असीम और अनंत हैं। ईश्वर संसार की नैतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं और जीवन के कर्मफल को निर्धारित करते हैं। भगवान का व्यक्तित्व उनकी असीमता से मेल खाता है, और वे भक्तों की विशेष कृपा करते हैं। गीता में भगवान के अवतारवाद को भी सत्य माना गया है।
शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत
शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में व्याख्यायित किया। उनका मानना था कि अज्ञान के कारण व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म को अलग मानता है।
रामानुज का विशिष्टाद्वैत वेदांत
रामानुज के दर्शन में ईश्वर ही परम सत्ता है। उनका ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है और अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।
आस्तिक और नास्तिक दर्शन
भारतीय दर्शन में दो प्रमुख वर्ग हैं: आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जबकि नास्तिक दर्शन इसे नकारता है। आस्तिक दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, और वेदांत आते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन में चार्वाक, जैन, और बौद्ध धर्म शामिल हैं।
चार्वाक दर्शन
चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। चार्वाकों का मानना है कि ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है, और वह केवल काल्पनिक है। उनका तर्क है कि जब ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता, तो उसकी उपासना भी निरर्थक है।
बौद्ध और जैन दर्शन
बौद्ध और जैन दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं माना गया, बल्कि उन्हें एक उद्धारक के रूप में देखा गया। जैन धर्म में भी ईश्वर का अस्तित्व नकारा गया, और यहां तीर्थंकरों को सर्वोच्च स्थान दिया गया।
न्याय और वैशेषिक दर्शन
न्याय और वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई प्रमाणों का उपयोग किया गया है। न्याय-दर्शन में ईश्वर को विश्व का स्रष्टा और पालक माना गया है, और उसे कार्यों के फल देने वाला माना गया है। वैशेषिक में भी ईश्वर को एक चैतन्य आत्मा के रूप में माना गया है, जो सृष्टि का संचालन करता है।
सांख्य और योग दर्शन
सांख्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर कुछ मतभेद हैं, जबकि योग दर्शन में ईश्वर को एक सर्वोच्च व्यक्तित्व माना गया है। योग-दर्शन में ईश्वर को ध्यान और भक्ति का विषय माना गया है।
मीमांसा दर्शन
मीमांसा दर्शन में ईश्वर को एक तुच्छ स्थान दिया गया है। यहां धर्म और कर्म के आधार पर सृष्टि की व्याख्या की जाती है, और देवताओं को केवल बलि और पूजा के माध्यम से महत्व दिया गया है।
अद्वैत वेदान्त और विशिष्टाद्वैत वेदान्त
शंकर के अद्वैत वेदान्त में ईश्वर का स्थान व्यावहारिक सत्य के रूप में है, जबकि ब्रह्म को पारमार्थिक सत्य माना गया है। वेदांत के इस मत में ईश्वर का व्यक्तित्व और निराकार रूप दोनों सम्मिलित हैं। रामानुज के विशिष्टाद्वैत वेदान्त में ब्रह्म और ईश्वर को अभिन्न माना गया है, और उन्हें सगुण रूप में पूजा जाता है।
समसामयिक भारतीय दर्शन
समकालीन भारतीय दर्शन में भी ईश्वर के विचारों पर विस्तृत चर्चा की गई है। विवेकानंद, अरविंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने अपने दर्शन में ईश्वर को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उनके विचारों में ईश्वरवादी परंपरा की झलक मिलती है।
इस प्रकार, भारतीय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व, स्वरूप, और उसके साथ संबंध रखने वाली विभिन्न विचारधाराओं का समृद्ध इतिहास है, जो समय के साथ विकसित होता रहा है।