उपनिषदों का दर्शन (Philosophy of the Upanisads)
उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत (वेद-अंत) भी कहा जाता है। वेदांत, वेदों का अंतिम भाग या सार है । उपनिषदों को इस अर्थ में भी वेदांत कहा जाता है कि इनमें वेद की शिक्षाओं का सार है। ये समस्त वेदों के मूल हैं।
उपनिषद् शब्द के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यह शब्द उप, नि, और सद् के संयोजन से बना है। ‘उप’ का अर्थ है निकट, ‘नि’ का अर्थ है श्रद्धा, और ‘सद्’ का अर्थ है बैठना। उपनिषद् का अर्थ है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश के लिए श्रद्धापूर्वक बैठना। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के वार्तालाप भरे पड़े हैं। धीरे-धीरे उपनिषद् का अर्थ गुरु से पाया हुआ रहस्य हो गया। शंकराचार्य ने उपनिषद् का अर्थ ‘ब्रह्म ज्ञान’ कहा है। यह वह विद्या है जिसके अध्ययन से मानव भ्रम से मुक्त हो जाता है और सत्य की प्राप्ति करता है। ज्ञान द्वारा मानव के अज्ञान का पूर्णतः नाश होता है।
उपनिषद् अनेक हैं। सामान्यतः उपनिषदों की संख्या 108 कही जाती है। इनमें से लगभग दस उपनिषदें मुख्य मानी जाती हैं: ईश, केन, प्रश्न, कठ, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, मुण्डक, छांदोग्य, और बृहदारण्यक। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में हैं। इनकी भाषा काव्यमयी है।
जहां तक उपनिषदों के रचयिता का संबंध है, हमें यह कहना पड़ता है कि इनके रचयिता कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं हैं। एक ही उपनिषद में कई शिक्षकों का नाम आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि एक उपनिषद किसी एक लेखक की कृति नहीं है। इन महान विचारकों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, इसका कारण उनका आत्मख्याति के प्रति अत्यधिक उदासीन होना कहा जाता है।
उपनिषद दार्शनिक और धार्मिक विचारों से परिपूर्ण हैं। लेकिन उपनिषदों का स्वरूप क्रमबद्ध दर्शन जैसा नहीं है। यही कारण है कि उपनिषदों के दार्शनिक विचारों को एकत्रित करने में कठिनाई होती है।
उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान निहित हैं। एक उपनिषद् में एक विचार का उल्लेख है तो दूसरी उपनिषद् में अन्य विरोधी विचार की चर्चा है। यही कारण है कि विभिन्न विचारों की पुष्टि के लिए उपनिषदों से श्लोक भाष्यकारों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं। इस प्रकार विरोधाभासी बातों की पुष्टि उपनिषदों के श्लोकों द्वारा होती है।
इससे उपनिषदों का दार्शनिक पक्ष गौण नहीं होता, बल्कि और भी सशक्त और प्रभावोत्पादक बनता है। दार्शनिक पक्ष ही उपनिषद की अमूल्य निधि है।
उपनिषद् और वेदों की विचारधारा में अंतर
उपनिषदें वेद के कर्मकाण्ड के विरुद्ध प्रतिक्रिया हैं। यही कारण है कि वेद की विचारधारा और उपनिषद की विचारधारा में महान् अन्तर दीखता है।
वेदों का आधार कर्म है, और उनमें यज्ञ की विधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके विपरीत, उपनिषदों का आधार ज्ञान है, और उनका मुख्य उद्देश्य जीवन से संबंधित गहन चिंतन और चरम तत्व (Ultimate Reality) के बारे में विचार करना है।
उपनिषदों में चरम तत्व के विषय में विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। ये मूलतः दर्शन-शास्त्र हैं, जिनमें गहन तात्त्विक विवेचन देखने को मिलता है।
वेद और उपनिषद के दृष्टिकोण का अंतर:
- वेदों के ऋषि: वेदों के ऋषिगण बहुदेववादी हैं। उनकी दृष्टि प्रकृति पर केंद्रित रहती है, और वे प्रकृति के विभिन्न रूपों को उपासना का विषय मानते हैं। वे प्रकृति को ही अपने कर्म और भक्ति का केंद्र बनाते हैं।
- उपनिषदों के ऋषि: इसके विपरीत, उपनिषदों के ऋषिगण प्रकृति के बजाय आत्मा को केंद्र मानते हैं। वे आत्मा का साक्षात्कार करने और उसके माध्यम से ईश्वर को अनुभव करने की अभिलाषा रखते हैं। उपनिषदों के ऋषियों ने ईश्वर को आत्मा में देखा है।
इस प्रकार, वैदिक धर्म बाह्यमुखी (Extrovert) है, जबकि उपनिषदों का धर्म अंतर्मुखी (Introvert) है।
जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण:
- वेद: वेदों के ऋषिगण संसार के भोग-विलास और ऐश्वर्य के प्रति जागरूक रहते हैं। उनका दृष्टिकोण आशावादी है।
- उपनिषद: इसके विपरीत, उपनिषदों के ऋषिगण संसार के भोग-विलास और ऐश्वर्य के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। उनके विचारों में एक गहन संवेदना और आध्यात्मिक निराशा की झलक मिलती है।
इस प्रकार, उपनिषदों में कहीं-कहीं निराशावादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, जो उन्हें वेदों से भिन्न बनाती है।
उपनिषदों का महत्त्व
उपनिषदों का भारतीय दर्शन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का मूल स्त्रोत उपनिषद् है। बब्लूम फील्ड के अनुसार, “नास्तिक बौद्धमत को छोड़कर, हिंदू विचारकों का ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण अंग नहीं है जिसका आधार उपनिषदों में न हो।”
उपनिषदों में आस्तिक मत (जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, अद्वैत वेदांत, और विशिष्टाद्वैत वेदांत) और नास्तिक मत (जैसे जैन और बौद्ध) के लगभग सभी मुख्य सिद्धांत निहित हैं। उदाहरणस्वरूप:
- बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का आरंभिक रूप कठोपनिषद में मिलता है, जहाँ मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को लेकर शंका व्यक्त की गई है।
- बुद्ध के दुःखवाद और क्षणिकवाद के सिद्धांत, जैसे “सर्वं दुःखम्” और “सर्वं क्षणिकम्,” का आधार भी उपनिषदों में मिलता है।
- सांख्य दर्शन के त्रिगुणमय प्रकृति का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है।
- इसी उपनिषद में योग के अष्टांग मार्ग का भी उल्लेख है।
- शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म और आत्मा-ब्रह्म संबंधी सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में पाए जाते हैं।
- मायावाद का सिद्धांत भी उपनिषदों में यत्र-तत्र मिलता है।
- रामानुज का दर्शन भी उपनिषदों पर आधारित है।
इस प्रकार, समस्त भारतीय दर्शन का बीज उपनिषदों में निहित है। उपनिषदों की महत्ता इस तथ्य से भी प्रकट होती है कि उन्होंने भारतीय दार्शनिकों को सदैव मार्गदर्शन दिया है। उनका उद्देश्य मानव आत्मा को शांति प्रदान करना है।
इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत में महान क्रांतियाँ हुईं, तब-तब दार्शनिकों ने उपनिषदों से प्रेरणा ग्रहण की। संकट के समय उपनिषदों ने मानवता का नेतृत्व कर अपना अपूर्व योगदान दिया है। आज भी, जब दर्शन और धर्म अथवा दर्शन और विज्ञान के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, तो उपनिषदें विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित कर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
प्रो. रानाडे का यह कथन सत्य प्रतीत होता है: “उपनिषद् हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो मानव की दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को एक साथ पूरा कर सके।”
उपनिषदों ने न केवल भारतीय विचारकों को प्रेरित किया है, बल्कि पाश्चात्य विचारकों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। शोपेनहावर जैसे दार्शनिक ने उपनिषदों से प्रकाश प्राप्त किया। महात्मा गांधी, अरविंद, विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और डॉ. राधाकृष्णन जैसे भारतीय मनीषी भी उपनिषदों से प्रेरित हुए। इसी कारण उपनिषदों को “विश्व-ग्रंथ” का स्थान प्राप्त है।
भारतीय दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, और उपनिषद इस अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक भारतीय दर्शन में अध्यात्मवाद की धारा प्रवाहित होगी, तब तक उपनिषदों का महत्व जीवित रहेगा। अतः उपनिषदों का महत्व शाश्वत है।
ब्रह्म-विचार
उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है। ब्रह्म एकमात्र सत्य, सत्ता और समस्त सृष्टि का सार है। इसे विश्व का आधार और आत्मा माना गया है। ‘ब्रह्म’ शब्द ‘बृह्’ धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है ‘विस्तार’ या ‘विकास’। ब्रह्म वह है जिससे समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें वह स्थित रहता है और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है।
उपनिषदों में ब्रह्म को दो रूपों में देखा गया है:
परब्रह्म (निर्गुण ब्रह्म):
- यह असीम, निर्गुण, निविशेष, और निष्प्रपंच है।
- यह उपासना का विषय नहीं है क्योंकि यह सभी गुणों और विशेषताओं से परे है।
- इसकी व्याख्या ‘नेति-नेति’ (न यह, न वह) कहकर की गई है।
- यह स्थिर, कालातीत और अपरिवर्तनशील है।
अपरब्रह्म (सगुण ब्रह्म):
- यह ससीम, सगुण, सविशेष और सप्रपंच है।
- यह उपासना का विषय है और ईश्वर के रूप में समझा जाता है।
- इसकी व्याख्या ‘इति-इति’ (यह भी, वह भी) कहकर की गई है।
हालाँकि, परब्रह्म और अपरब्रह्म एक ही ब्रह्म के दो पक्ष हैं।
ब्रह्म के गुण और स्वरूप
- अद्वितीयता: ब्रह्म अद्वितीय है और द्वैत (ज्ञाता और ज्ञेय) से परे है।
- कालातीत: ब्रह्म समय के अधीन नहीं है, लेकिन समय का आधार है। यह त्रिकाल (भूत, वर्तमान, भविष्य) से परे है।
- दिक्-शून्य: ब्रह्म दिशाओं की सीमाओं से मुक्त है, परंतु दिशाओं का आधार है।
- अचल और गतिशील: ब्रह्म स्थिर होकर भी सब कुछ चलायमान रखता है। यह अचल होने के बावजूद गतिमान प्रतीत होता है।
- अजर-अमर: ब्रह्म परिवर्तन और मृत्यु के अधीन नहीं है। यह शाश्वत और नित्य है।
- सच्चिदानंद: ब्रह्म का स्वरूप सत् (अस्तित्व), चित् (चेतना), और आनंद (परमानंद) है। यह व्यावहारिक जगत् के सत्, चित् और आनंद से परे है।
शंकर और रामानुज का दृष्टिकोण
- शंकराचार्य: उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण रूप (परब्रह्म) पर बल दिया। उनके अनुसार, ब्रह्म निर्विशेष और अद्वैत (एकता) का प्रतिनिधित्व करता है।
- रामानुजाचार्य: उन्होंने सगुण ब्रह्म (अपरब्रह्म) पर बल दिया। उनके अनुसार, ब्रह्म गुणों से युक्त और भक्तिपूर्ण उपासना का विषय है।
ब्रह्म और आत्मा का संबंध
उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा (जीव) को एक ही तत्व माना गया है। आत्मा, जो चेतना का स्रोत है, ब्रह्म का ही अंश है। यही कारण है कि उपनिषदों का लक्ष्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता।
ब्रह्म का महत्व
उपनिषदों में ब्रह्म को संपूर्ण विश्व और जीवन का मूल तत्व माना गया है। यह असीम, अनंत और अपरिवर्तनशील है। इसके साथ ही, उपनिषदों ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्म ही सत्य है, और उसकी प्राप्ति से ही जीवन का अंतिम उद्देश्य पूरा होता है।
आत्मा का स्वरूप:
उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आत्मा को ब्रह्म का ही सूक्ष्म और वैयक्तिक रूप कहा गया है। ‘तत्त्व मसि’ (बही तू है) ‘अहं ब्रह्मास्मि’ (मैं ब्रह्म हूँ) आदि वाक्य आत्मा और ब्रह्म की_ एकता पर बल देते है। शंकर ने भी आत्मा और ब्रह्म के अभेद पर जोर दिया है। आत्मा मूल चैतन्य है, जो ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। यह मूल चेतना का आधार है और नित्य तथा सर्वव्यापी है। आत्मविचार उपनिषदों का केन्द्रीय तत्व है, और यही कारण है कि आत्मा की गहरी व्याख्या उपनिषदों में मिलती है। प्रजापति और इन्द्र के संवाद में, प्रजापति आत्मा के स्वरूप पर चर्चा करते हुए यह बताते हैं कि आत्मा न तो शरीर है, न ही वह वह तत्व है, जिसकी अनुभूति स्वप्न या निद्रा की अवस्था में होती है। आत्मा उन सभी अवस्थाओं में मौजूद होने के बावजूद, उनसे परे है।
जीव और आत्मा का भेद:
उपनिषदों के अनुसार जीव और आत्मा में भेद है। जीव वैयक्तिक आत्मा (Individual self), आत्मा परम आत्मा (Supreme self) है। जीव और आत्मा उपनिषद् के अनुसार एक ही शरीर में अन्धकार और प्रकाश की तरह निवास करते हैं। जीव, कर्म के फलों को भोगता है और सुख दुःख अनुभव करता है। आत्मा, इसके विपरीत कूटस्थ है। जीव अज्ञानी है। अज्ञान के फल स्वरूप उसे बन्धन और दुःख का सामना करना पड़ता है। आत्मा ज्ञानी है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से जीव दुःख एवं बन्धन से छुटकारा पा जाता है। जीवात्मा कर्म के द्वारा, पुष्य, पाप का अर्जन करता है और उनके फल भोगता है। लेकिन आत्मा कर्म और पाप पुण्य से परे है। वह जीवात्मा के अन्दर रहकर भी उसके किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। आत्मा जीवात्मा के भोगों का उदासीद साक्षी है। जीव और आत्मा दोनों को उपनिषद् में नित्य और अज माना गया है। उपनिषदों में जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। वह शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि से अलग तथा इनसे परे है। वह ज्ञाता, कर्ता तथा भोक्ता है। उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार नियमित होता है। जीवात्मा अनन्त ज्ञान से शून्य है।
जीवात्मा की चार अवस्थाएँ:
- जाग्रत अवस्था (Waking State): जाग्रत अवस्था में जीवात्मा विश्व कहलाता है। वह वाह्य इन्द्रियों द्वारा सांसा रिक विषयों का भोग करता है।
- स्वप्न अवस्था (Dream State): स्वप्न की अवस्था में जीवात्मा ‘विश्व’ कहलाता है। वह आन्तरिक सूक्ष्म वस्तुओं को जानता है और उनका भोग करता है।
- सुपप्ति अवस्था (Deep Sleep State): सुपप्ति की अवस्था में जीवात्मा ‘प्रज्ञा’ कहलाता है जो कि शुद्ध चित् के रूप में विद्यमान रहता है। इस अवस्था में वह आन्तरिक या बाह्य वस्तुओं को नहीं देखता है।
- तुरीय अवस्था (Transcendental State): तुरीयावस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है। वह शुद्ध चैतन्य है। तुरीयावस्था की आत्मा ही ब्रह्म है।
पाँच कोष (Sheaths of Self):
तैतिरीय उपनिषद् में आत्मा के पाँच आवरणों का वर्णन किया गया है, जो इसे भौतिक और मानसिक सीमाओं में बाँधते हैं:
- अन्नमय कोष: स्थूल शरीर, जो भोजन पर निर्भर करता है।
- प्राणमय कोष: अन्नमय कोष के अन्दर प्राणमय कोष है। यह शरीर में गति देने बाली प्राण शक्तियों से निर्मित हुआ है। यह प्राण पर आश्रित है।
- मनोमय कोष: प्राणमय कोष के अन्दर मनोमय कोष है। यह मन पर निर्भर है। इसमें स्वार्थमय इच्छायें हैं।
- विज्ञानमय कोष: मनोमय कोष के अन्दर ‘विज्ञान मय कोष’ है। यह दुद्धि पर आश्रित है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद करने बाला ज्ञान निहित है।
- आनन्दमय कोष: विज्ञानमय कोष के अन्दर आनन्दमय कोष है। यह ज्ञाता और शेय के भेद से शून्य चैतन्य है। इसमें आनन्द का निवास है। यह पारमाथिक और पूर्ण है। यह आत्मा का सार है न कि कोष। यही ब्रह्म है। इस आत्मा के ज्ञान से जीवात्मा बन्धन से छूटकारा पा जाता है। इस ज्ञान का आवार अपरोक्ष अनुभूति है। चूंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप आनन्दमय है इसलिये अात्मा को ‘सच्चि दानन्द’ भी कहा गया है। आत्मा शुद्ध सत्, चित् और आनन्द का सम्मिश्रण है। आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं के विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा सत् + चित् + आनन्द है।
आत्मा और ब्रह्म
उपनिषद् दर्शन में आत्मा और ब्रह्म को अद्वैत (अभिन्नता) के सिद्धांत के आधार पर एक ही सत्य के दो पहलू माना गया है। आत्मा और ब्रह्म के संबंध में उपनिषदों ने यह स्पष्ट किया है कि आत्मा व्यक्तिगत अनुभव का आधार है, जबकि ब्रह्म सार्वभौमिक वास्तविकता है। दोनों का तादात्म्य उनकी एकात्मता और परस्पर अभिन्नता पर आधारित है।
आत्मा और ब्रह्म की तादात्म्यता:
- महावाक्य: उपनिषदों के चार प्रमुख महावाक्य आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता को प्रमाणित करते हैं:
- तत्त्वमसि (वही तू है) – ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान।
- अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ) – आत्मा स्वयं ब्रह्म है।
- अयमात्मा ब्रह्म (यह आत्मा ब्रह्म है) – आत्मा और ब्रह्म की एकता।
- प्रज्ञानं ब्रह्म (ज्ञान ही ब्रह्म है) – ब्रह्म शुद्ध चेतना है।
शंकराचार्य का दृष्टिकोण:
आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म की तादात्म्यता पर जोर दिया। उनके अनुसार, आत्मा (जीव) और ब्रह्म (परमात्मा) में भेद केवल अज्ञान (अविद्या) के कारण है। जब यह अज्ञान दूर होता है, तो जीवात्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है।
आत्मा और ब्रह्म के विवरण उपनिषद् में एक जैसे हैं। दोनों को चरम तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। दोनो को सत् + चित् आनन्द अर्थात् ‘सच्चिदानन्द’ माना गया है। दोनों को सत्यम्, ज्ञानम् अनन्तम् कहा गया है। दोनों को सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् माना गया है। दोनों के आनन्दमय रूप पर जोर दिया गया है। दोनों को सभी शान का आधार बतलाया गया है।
आत्मा और ब्रह्म की अवस्थाएँ:
उपनिषदों में आत्मा की चार अवस्थाओं को ब्रह्म के विभिन्न रूपों से जोड़ा गया है:
- जाग्रत अवस्था: आत्मा का जाग्रत रूप ब्रह्म के विराट रूप के समान है।
- स्वप्न अवस्था: आत्मा का स्वप्न रूप ब्रह्म के हिरण्यगर्भ स्वरूप से मेल खाता है।
- सुषुप्ति अवस्था: आत्मा का सुषुप्ति रूप ब्रह्म के ईश्वर रूप के तुल्य है।
- तुरीय अवस्था: आत्मा की तुरीय अवस्था ब्रह्म का परब्रह्म स्वरूप है।
डॉ. राधाकृष्णन और अन्य विचारक:
डॉ. राधाकृष्णन ने उपनिषद् दर्शन में आत्मा और ब्रह्म के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही तत्त्व के दो पक्ष हैं। प्लेटो और हीगल जैसे दार्शनिकों से पहले, उपनिषदों ने आत्मा और ब्रह्म की एकात्मकता का दर्शन प्रस्तुत किया।
ड्यसन ने भी उपनिषदों के इस योगदान को सराहा और कहा कि उपनिषद् विचारकों ने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि आत्मा, ब्रह्म के रूप में, समस्त घटनाओं और प्रकृति के भीतर व्याप्त है।
जगत्-विचार: उपनिषद् दर्शन में जगत् की अवधारणा
ब्रह्म ही जगत् की उत्पत्ति का कारण है और वह ही इसका पालन करता है, अंततः वह ब्रह्म में समाहित हो जाता है। वृहद्वारण्यक उपनिषद् में यह कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है और फिर उसी में समाहित हो जाता है। देश, काल, प्रकृति आदि ब्रह्म के आवरण हैं, क्योंकि हर स्थान में ब्रह्म व्याप्त है। जैसे नमक पानी में मिलकर उसे पूरी तरह से प्रभावित करता है, वैसे ही ब्रह्म सभी पदार्थों में समाहित हो जाता है।
उपनिषदों में कई स्थानों पर जगत् को ब्रह्म का विकास माना गया है, और इस विकास का क्रम भी उपनिषदों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सबसे पहले ब्रह्म से आकाश का विकास होता है, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि और इसी तरह से अन्य तत्वों का विकास होता है।
इसके अतिरिक्त, उपनिषदों में जगत् के पाँच स्तरों का उल्लेख भी किया गया है, जिसे ‘पञ्चकोष’ कहा जाता है। ये पाँच कोष हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय। अन्नमय कोष भौतिक पदार्थों से संबंधित है, प्राणमय कोष में जीवन शक्ति समाहित है, मनोमय कोष में मानसिक तत्व है, विज्ञानमय कोष बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, और आनन्दमय कोष में सर्वोच्च आनंद और ब्रह्म का अनुभव किया जाता है।
उपनिषदों में सृष्टि की व्याख्या सादृश्यता और उपमाओं के माध्यम से की गई है। जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैं, सोने से आभूषण बनते हैं, मोती से चमक उत्पन्न होती है, और बांसुरी से ध्वनि निकलती है, वैसे ही ब्रह्म से सृष्टि होती है। मकड़े की उपमा से भी जगत् के विकास को समझाया गया है, जैसे मकड़ा अपने शरीर से जाले बुनता है, वैसे ही ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है।
उपनिषदों में सृष्टि को एक लीला के रूप में देखा गया है, जो आनंददायक खेल की तरह है। यहाँ तक कि उपनिषदों में कहीं भी विश्व को भ्रमजाल के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है। उपनिषदों के ऋषि प्राकृतिक जगत् के भीतर जीवन यापन करते रहे और कभी भी इस जगत् से पलायन करने का विचार नहीं किया। इस दृष्टिकोण से, उपनिषद् जगत् से भागने की बजाय उसे समझने और अनुभव करने की शिक्षा देता है।
माया और अविद्या
उपनिषदों में माया और अविद्या का विचार भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शंकर के माया और अविद्या सिद्धांत के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें बौद्ध दर्शन से लिया है, लेकिन यदि यह सत्य न हो, तो यह कहना उचित होगा कि माया और अविद्या के विचार शंकर के मन की उपज हैं। दोनों ही विचार भ्रमित करने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन शंकर ने माया और अविद्या से संबंधित धारणा उपनिषदों से ग्रहण की है। प्रो. राष़डे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक A Constructive Survey of Upanisadic Philosophy में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि माया और अविद्या के विचार का स्रोत उपनिषद ही हैं।
उपनिषदों में माया और अविद्या का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:
- श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है कि ईश्वर मायाविन है। माया ईश्वर की शक्ति है, जिसके द्वारा वह सृष्टि का निर्माण करता है।
- छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है, जबकि सभी वस्तुएं केवल नाम और रूप का भेद हैं।
- प्रश्न उपनिषद् में यह कहा गया है कि हम ब्रह्म को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम भ्रम की अवास्तविकता से मुक्त नहीं होते।
- वृहदारण्यक उपनिषद् में अवास्तविकता को असत् और अंधकार से जोड़ा गया है।
- छान्दोग्य उपनिषद् में विद्या को शक्ति और अविद्या को अशक्ति से तुलना की गई है।
बन्धन और मोक्ष
बन्धन और मोक्ष का विचार भी उपनिषदों में प्रमुख है, जैसे अन्य भारतीय दर्शनों में है। मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। बन्धन का कारण अविद्या है, क्योंकि अविद्या से ही अहंकार उत्पन्न होता है, और यही अहंकार जीवों को बन्धन में डालता है। इस अहंकार के प्रभाव में जीव अपने इन्द्रिय, मन, बुद्धि या शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। बन्धन की अवस्था में जीव को जगत् और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रहता है, और इसके कारण वह असत्, अवास्तविक और क्षणिक पदार्थों को यथार्थ समझने लगता है। बन्धन को उपनिषदों में ‘ग्रन्थि’ कहा गया है, जिसका अर्थ है ‘बन्ध जाना’।
मोक्ष के लिए विद्या आवश्यक है, क्योंकि विद्या से ही अहंकार का नाश होता है और जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। विद्या के विकास के लिए उपनिषदों में नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह प्रमुख हैं। मोक्ष की अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, जैसे नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। इस प्रकार, मोक्ष ऐक्य का शान है, जहाँ जीव ब्रह्म से एक होकर अनन्त आनंद का अनुभव करता है।
मोक्ष की अवस्था को उपनिषदों में आनंदमय माना गया है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं आनंदमय है। इसलिए, मोक्ष की अवस्था भी आनंदपूर्ण होती है, जहाँ जीव और ब्रह्म के बीच सभी भेद मिट जाते हैं और एकता की अनुभूति होती है।


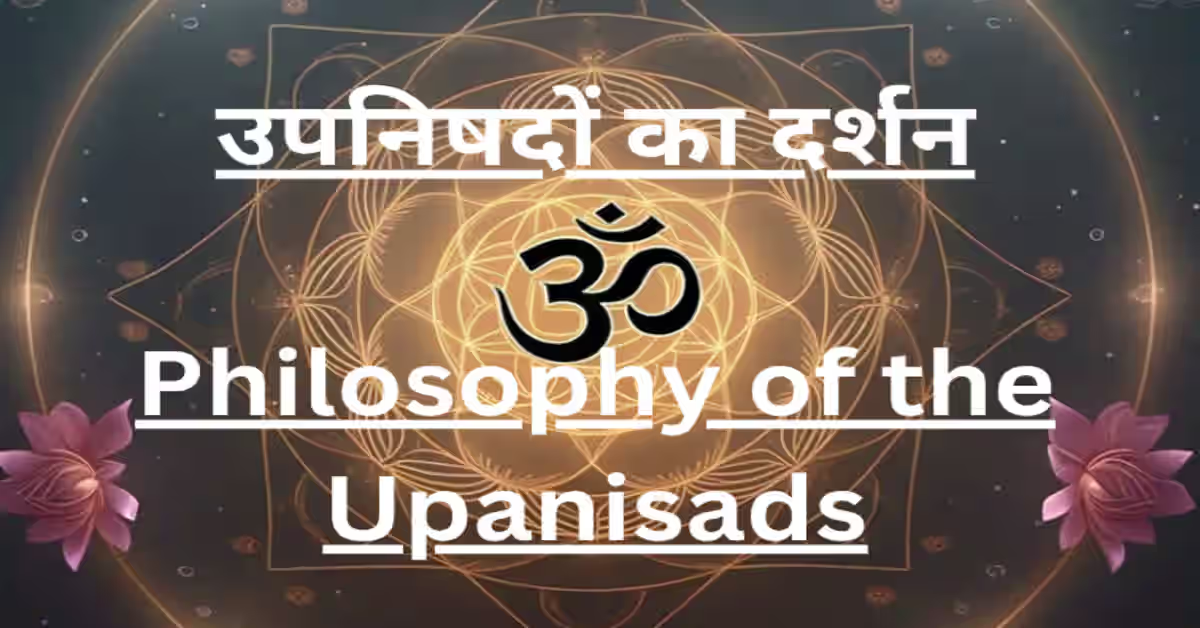

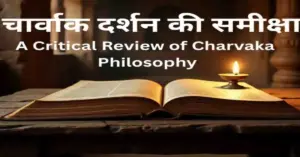

Pingback: गीता का दर्शन (Philosophy Of Bhagavad Gita) - Shivoham